दिल में क्या झरना है !
मैंने जिस एक पात्र पर सबसे अधिक लिखा वह हैं ‘गंठी दादी’ । बार-बार लिखता रहा फ़िर भी हर बार कुछ न कुछ छूट ही जाता रहा । न जाने कितनी ऐसी बातें हैं जो लिखकर उठने के तुरंत बाद अंदर से उछलकर बाहर आ जातीं । खून के मतलबी रिश्तों से अलग न जाने ये कौन-सा रिश्ता है जिसकी संवेदनाएँ झरने-सी बह रही हैं । जब-जब दादी के बारे में सोचता हूँ या गाँव-गिराँव में उनके बारे में सुनता हूँ या देखता हूँ, हर बार कुछ नया सामने आ जाता है । एक नए स्वरूप में भी । अक्सर मुक्तिबोध की एक कविता की कुछ पंक्तियाँ याद हो आती हैं –
“जाने क्या रिश्ता हैं, जाने क्या नाता हैं
जितना भी ऊँड़ेलता हूँ भर-भर फिर आता हैं
दिल में क्या झरना है?
मीठे पानी का सोता हैं
भीतर वह, ऊपर तुम
मुसकता चाँद ज्यों धरती पर रात-भर
मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा हैं !”
दादी के साथ जुड़ी मेरी संवेदनाओं पर आधारित शब्दचित्र ‘गंठी भंगिनियां’ लिखे आज करीब दस-बारह साल हो गए हैं । ‘दलित अस्मिता’ में ज्यौं का त्यौं छपा भी । बावजूद इसके न जाने क्या छूट गया था जो उसी शीर्षक से एक स्वतंत्र किताब के रूप में सामने आया । इसके बाद आलोचकों / समीक्षकों की कलम भी उस पर चली लेकिन संवेदनाओं का विस्तार ऐसा था कि ‘सिमट’ नहीं पाया । इसके बाद फ़ेसबुक इत्यादि सामाजिक नेटवर्क पर मैंने कई-कई पोस्टें लिखीं, जिन पर न जाने कितने लोगों की प्रतिक्रियाएँ आईं और संवेदना का जो जुड़ाव था वह बढ़ता ही गया ।
दादी से जुड़ी संवेदनाओं को समेटने के क्रम में अंदर जो जमा था सैकड़ों-हजारों वर्षों की परंपरा से, टुकड़े-टुकड़े होता रहा । सामाजिक मर्यादा और आदर्श का मुलम्मा उतरता रहा । सामाजिक मुक्ति की राह सहज से सहजतर होती गई । यहाँ तक कि निराला जी के शब्दो में ‘ब्राह्मण समाज में ज्यौं अछूत’ वाली स्थिति भी आ पहुँची । ... लेकिन इस स्थिति ने अंदर से इतनी मज़बूती प्रदान की कि दिखावटी भार बालू-सा झर गया ।
मेरी किताब छप चुकी थी । जगह-जगह उसका विमोचन हो रहा था । समीक्षा / आलोचना का दौर भी चालू हो गया था । वाह-वाही और प्रश्नचिन्ह साथ-साथ मिल रहे थे । सवर्ण और दलित लेखक / विद्वान अपनी-अपनी तरह से पुस्तक पर बात कर रहे थे । बावजूद इसके मैं अभी तक वह प्रसन्नता नहीं महसूस कर पा रहा था जो एक लेखक को उसकी किताब के विमोचन के दौरान मिलती है । मेरा मन नहीं माना और मैं नौकरी से छुट्टी लेकर घर आया और दादी के साथ उनके हाथों ही घर पर किताब का विमोचन किया । इसी पर एक पोस्ट लिखी थी । बड़ी मज़ेदार थी । प्रस्तुत है –
“मेरी दोनों किताबें आने के बाद मेरी सबसे अधिक उत्सुकता ‘गंठी भंगिनिया’ किताब दादी को दिखाने की थी । यह किताब उनके जीवन से प्रेरित है । कल मैं घर था और इत्तफाकन मेरे मिलने से पहले ही दादी घर आईं किसी काम को लेकर । मैंने दादी को किताब दिखाई और किताब के कई प्रसंग (दृश्य पढ़कर सुनाए । वह ऐसे सुन रही थीं जैसे किसी और की कहानी सुन रही हों । मैंने देखा उस समय दादी के चेहरे पर गंभीर एकाग्रता थी । मैंने दादी से कुछ बोलने को कहा तो जैसे वह स्वप्न से बाहर आई हों । कहने लगीं ‘लल्ला आज तक मुझे लगा ही नही कि मैं भी इस समाज का हिस्सा हूँ । इसलिए कभी इस सामाजिक ऊँच-नीच के बारे में सोचा ही नहीं । आज पहली बार लगा जैसे कि मैं भी इंसान हूँ । आप सबकी तरह ।’ यह सब बातें दादी ने कहीं शून्य में खोई हुए-सी अवस्था में अपनी भाषा में कहीं । वह आगे कहने लगीं कि ‘लल्ल जब तुम बहू (मेरी माँ की ओर देखते हुए) के पेट में थे तब तुम्हारी दादी बहू से कुछ नाराज़ चल रही थीं । हमें अच्छे से याद है वह दिन जब तुम्हारी माँ प्रसव से तड़प रही थीं और कोई उनके पास बैठने वाला नहीं था, तब मैं पूरे दिन उनके पास रहकर उन्हें दिलासा देती रही । मैं वह दिन कभी नहीं भूल सकती ।’ दादी कुछ ‘इमोशनल’ हो चलीं । बातों ही बातों में उन्होंने गाँव से आनगाँव तक के पचासों लोगों के नाम गिनाए जो दादी के ही हाथों पैदा हुए थे । एक वैद्य का हुनर और एक माँ-सी ममता रखने वाली यह दादी आज भी अस्पृष्य ही मानी जाती हैं । मैंने समाज के नियमों को तोड़ते हुए जब उन्हें गले लगाया तो मेरा घर-परिवार से लेकर समाज तक विरोध हुआ, पर मैं प्रसन्न हूँ कि मैं दादी को यह समझा सका कि वह भी सबकी तरह इंसान ही हैं । हमने आज खूब सारी बातें कीं । घर में एक साथ बराबर में बैठकर चाय पीते हुए । एक साथ मेरे पिता जी, माता जी, भाई-बहने, सीमा, मैं और शब्द । और हम सबके साथ में ‘गंठी भंगिनिया’ अर्थात दादी । . . . और इस प्रकार से दादी ने अपने जीवन की प्रेरणा पर आधारित मेरी सबसे बेहतरीन किताब ‘गंठी भंगिनिया’ का लोकार्पण किया ।”
इस रिपोर्ट पर खूब प्रतिक्रिया आई लोगों की । सैकड़ो लोगों की प्रतिक्रियाएँ आईं । सहज मित्र, साहित्यकार, समीक्षक, आलोचक, साथी सब के सब मेरी इस मुहिम के साथ खड़े होते हुए दिखाई दिए । बावजूद इसके हमारे कुछ ‘अपने’ कहे जाने वाले हमसे कुंठित भी हो गए । उनकी कुंठा केवल इस बात को लेकर हुई कि अब तक ‘नायकत्त्व’ केवल सवर्ण समाज के पात्र पाते चले आ रहे थे तो मैंने स्वयं सवर्ण होकर भी एक दलित पात्र को अपने लेखन का आलंबन क्यों बनाया और स्वयं उसके साथ उठना-बैठना क्यों बनाए हुए हूँ ।
मेरी आदत में ही आ चुका था कि मेरा जब-जब विरोध हुआ, मुझे शक्ति मिली । लड़ने का उत्साह उत्पन्न हुआ । और यह आक्रोष मेरे लेखन की बुनियाद भी बना । मेरे इसी आक्रोश ने मुझे फ़ेसबुक पर क्रोधपूर्ण ‘पोस्ट’ लिखबा दी ।
“आज इक्कीसवीं सदी में भी तमाम सवर्ण स्वयं को बदल नहीं पाए हैं । इस दलित महिला को नायक बनाकर लिखी गई मेरी किताब ‘गंठी भंगिनियां’ की आलोचना कुछ सवर्ण बंधु यह कहकर करते हैं कि ‘तुम्हें इस भंगिनियां के अलावा कोई विषय नहीं मिला किताब लिखने को ?’ मेरे घर में किताब का विमोचन जब इन दादी ने किया, उसके बाद तमाम लोग महज इस लिए नाराज़ हैं कि ‘एक ब्राह्मण के घर में एक मेहतर महिला कुर्सी पर बराबरी में बैठी है ।’ .... भाड़ में जाओ सब ।”
वास्तव में यह पोस्ट मेरे क्रोध की प्रतिक्रिया न होकर दादी के साथ मेरी ‘सह-संवेदना’ की सूचक थी । मैं उनके दर्द को लगातार महसूसने का प्रयास करता रहा ।
लगे हाथ एक स्वनामधन्य दलित लेखक ने भी राय दे डाली । मैंने उसको लिखा – “मेरा एक शब्दचित्र है ‘गंठी भंगिनियां’, जो मेरा जिया हुआ यथार्थ है । इसमें मेरे गाँव की ‘मेहतर दादी’ का जीवन संघर्ष है । छपी और खूब वाहवाही भी मिली । खूब फोन आए । सबने सराहना की । इधर एक बडे दलित साहित्यकार का फोन आया । खूब सराहना करने के बाद बोले – ‘भाई मानव जी कहानी बहुत अच्छी लगी फिर भी आगे यह ध्यान रखिए कि कहानी में दलित नायक हो और सवर्णों पर उनके साथ संघर्ष और जीत अवश्य दिखाई गई हो । वास्तविक अंबेडकरवाद यही है ।’ मैं अपने साहित्य में कल्पना और विचारों का सहारा केवल प्रवाहमयता के लिए ही लेता हूँ । शेष सब यथार्थ ही होता है । मेरी आंखों देखा सच ।”
संभवत: लेखक महोदय मुझे लेखक समझ बैठे थे । वह भी किसी ‘खांचे’ में बंधा हुआ । उनके लिए इन संवेदनाओं को समझना / महसूस करना संभव ही नहीं था । फ़िलहल मुझे इन पर क्रोध नहीं आया बल्कि मेरे लिए यह हास्य के ही पात्र रहे ।
इसी दौरान मैं ‘पिता’ बना । इतिहास ने अपने आपको एक बार फ़िर दोहराया । एक पोस्ट लिखी । पढ़िए । मज़ेदार बनी थी । फ़िर आगे बात करता हूँ ।
“हमारे घर एक प्रथा है - जन्म लेते ही बच्चे को बेचने की । जिया ने बताया था कि परिवार में मुझसे यह प्रथा चली थी । मुझे खरीदा था गंठी दादी ने । (हमारी गांव से लेकर इलाके तक इनको गंठी भंगिनिया नाम से पुकारा जाता है) मुझे इन दादी से बचपन से ही स्नेह रहा । मैंने उन्हें सनातनी समाज की कुरीतियों में फंसकर घुटते हुए देखा । जो देखा उसे लिखने का प्रयास भी किया । आज दादी उस स्थिति से काफी ऊपर आई हैं । जब भी हमें मिलती हैं तो उनके चेहरे पर वही मुस्कान पाता हूँ जो मेरे लिए सदा रहती है । अभी मेरा बेटा हुआ - शब्द । फिर से दादी द्वारा वही रीति दोहराई गई यानि कि बच्चे को खरीदकर अपना बनाया फिर वापस बच्चे की मां को धरोहर के रूप में सौंप दिया । चौंतीस वर्ष बाद दोहराई गई इस रीति ने एक बार फिर से पूरी कहानी कह डाली । मैं इन सबमें विश्वास नहीं रखता, लेकिन दादी ने जिस आग्रह से यह कार्य किया, वह अद्भुत था । दादी की गोद में बेटे 'शब्द' को देखकर मैं आनंदित हो उठा । ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा लिखा हुआ शब्दचित्र आज चरितार्थ हो गया हो और मैं एक बडी सामाजिक लडाई जीत गया हूँ । चौंतीस वर्ष बाद की इस घटना में नई बात यह कि आज कम से कम मेरे घर और दादी के बीच की जो सवर्ण-अवर्ण की दूरी थी, कम तर हुई है ।”
यह सब यूँ ही बीच-खूच चलता रहा । दादी अपनी संवेदनाओं की जड़ें मेरे अंदर मज़बूत करती रहीं । बावजूद इसके एक घटना मैं लिखने से बचता रहा, लेकिन कुलबुलाता रहा अंदर ही अंदर कि अवश्य लिखूँ । लोगों को बताऊँ कि उनके जीवन का एक दर्द यह भी है ।
दादी के एक लड़के और बाबा के मरने के बाद उनके लड़कों ने दादी की बेकद्री करनी आरम्भ कर दी । मैंने गाँव के लोगों से सुना कि उनका लड़का, जो देखने में दरिद्र और बेचारा-सा दिखता है, अपनी माँ को बात-बेबात पर अश्लील से अश्लील गालियाँ देता है । एक बार तो दादी एक जगह लेटे दिखीं तो किसी ने बताया कि ‘राजिन्दर ने घर से निकाल दिया है ।’ मेरा क्रोध सातवें आसमान पर जा पहुँचा । बावजूद इसके दादी ने अपनी सौगंध देकर उससे कुछ न कहने का वचन लिया । किसी तरह उनके लड़के को किसी के माध्यम से समझवाने का प्रयास किया लेकिन मैं चाहते हुए भी दादी के इस दर्द की दवा न बन सका ।
जब मैं दादी को लेकर शब्दचित्र और बाद में किताब लिख रहा था तो मैंने उसे शीर्षक दिया ‘गंठी भंगिनियां’ । इस शीर्षक को लेकर मैं सहज न था । ‘भंगिनियां’ शब्द संवैधानिक तो था ही नहीं, घृणास्पद भी था । जैसा कि बाद में पुस्तक पर समीक्षा लिखते हुए बजरंग बिहारी जी ने इंगित भी किया । बावजूद मैंने पूरी तरह सोच-समझकर यह शीर्षक दिया । तमाम दलित लेखकों से बात की । उनके राय ली । जातिगत संबोधन को लेकर उक्त शीर्षक से लिखी गई दलित लेखकों की किताबें पढ़ीं । किसी भी कीमत पर घृणा का भाव कम न हुआ । जबकि अधिकांश ने उक्त शीर्षक रखने के संबंध में अपनी दलील दी । मैंने केवल एक निस्कर्ष और भाव को अपने अंदर स्थान दिया । वह यह कि मैं उस सामाजिक और धार्मिक रूप से तिरस्कृत शब्द को जीवित रखना चाहता था, जिससे दर्द को जीवित रख सकूँ । समाज के उन लांछनों को जीवित रख सकूँ जिनको दादी ने जीवन भर जिया है ।
दादी के साथ मेरे संवेदनाओं का कोई अंत नहीं है । जितना लिखता जाता हूँ । उससे अधिक कहीं ‘रिसियाता’ जाता है । जब-जब भरता जाएगा । निकलता रहेगा । संवेदना का यह ‘सोता’ कभी समाप्त न होगा ।
सुनील मानव
02.06.2020

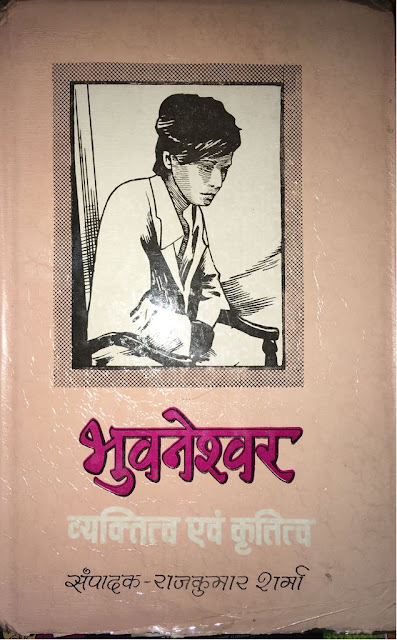
Comments
Post a Comment