छोटे शहर की समस्याएं और शाहजहाँपुर का रंगमंच सुनील ‘मानव’
छोटे शहरों की
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व बौद्धिक स्तर पर अनेक समस्याएं होती हैं। यह एक
ऐसा संक्रमण कालीन समाज होता है ,जहाँ कस्बाई प्रवृत्तियाँ पूरी तरह से छूटती नही हैं और
महानगरीय प्रवृतियाँ पूरी तरह से अस्तित्व में आ नहीं पाती। इसका चरित्र
अन्तर्विरोधात्मक होता है। नए मूल्य स्थापित नहीं हो पाते और पुराने मूल्य छूट
नहीं पाते। प्रगति और परम्परा के बीच बनता-बिगड़ता संतुलन इसे एक ऐसा चरित्र प्रदान
करता है, जो सामान्य संकल्पना से बिल्कुल भिन्न होता है। बाज़ार और
विज्ञापनवादी संस्कृति के प्रभाव ने इसकी प्रवृतियों को और उलझा दिया है।
भूमण्डलीकरण और प्रछन्न आर्थिक उपनिवेशवाद ने छोटे शहरों के चरित्र को बुरी तरह
प्रभावित किया है। कुल मिलाकर तमाम तरह के सामाजिक - आर्थिक दवाबों से छोटे शहरों
का स्वरूप विशिष्ट और जटिल हो जाता है।
छोटे शहरों का समाज संक्रमणकालीन होता है। इसका निर्माण तमाम तरह की विरोधी
प्रवृतियों से होता है। शिक्षा, स्वास्थ तथा रोजगार का स्तर जहाँ एक ओर प्रगति की सूचना
देता है, वहीं दूसरी ओर अंधविश्वास,
आर्थिक असमानता तथा तीव्र जनसंख्या वृद्धि इसके विकास की
अवरुद्धता की ओर संकेत करते हैं। विज्ञापनी चकाचौंध से जहाँ एक ओर बौद्धिकता और
विचारशीलता के विकास पर अंकुश लग जाता है,
वहीं दूसरी ओर महानगरों की दौड़ - भाग भरी जिन्दगी की
अपेक्षा ठहराव और मानसिक संतुष्टि बौद्धिकता और विचारशीलता के लिए उर्वर शहरों की
प्रवृतियाँ भिन्न होती हैं। नौकरी की तलाश और अवसरों की अल्पता युवाओं के चरित्र
को एक अलग ही रूप देती है। शिक्षा का महत्व सिर्फ रोज़गार की प्राप्ति तक सीमित
होता है। ऐसे में उनके पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। सुरक्षित आजीविका की तलाश
उनकी वैचारिकता - प्रतिबद्धता का अवशोषण कर लेती है। अल्प साधन और असुरक्षित
वातावरण उन्हें पेट भरने के अथवा तड़क - भड़क भरे वातावरण के अनुकूल अपनी आवश्यकताओं
की पूर्ति के अलावा और कुछ न सोचने - करने
को विवश करता हैं। शिक्षा के उद्देश्य का केन्द्रण रोज़गार की ओर हो जाने के कारण
शिक्षा अपनी अर्थवत्ता खो देती है। अंधविश्वासों का जीवित रहना,
अनुदारता, साम्प्रदायिक व रूढ़िवादी सोच छोटे शहरों की अन्य विशेषताएं
हैं, किन्तु इन सबके बावजूद विकास की सर्वाधिक सम्भावनाएं इन्हीं क्षेत्रों में
होती हैं। वैचारिक विकास के लिए छोटे - शहरों का वातावरण अत्यंत उर्वर होता है।
छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः व्यापार व कृषि पर आधारित होती है। बड़ी
औद्योगिक इकाइयों के अभाव के कारण रोजगार की सहज सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पातीं।
लघु उद्योग धन्धे और कुटीर इकाईयां बड़ी इकाइयों के सामने पनप नहीं पाती हैं।
ग्राहक स्वयं अपने शहर की चीजों की गुणवत्ता पर संदेह करता है। मुख्यतः व्यापार के
माध्यम से ही छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था नियंत्रित होती है। कृषि उत्पादों तथा
कृषि सम्बंधी उद्योग-धन्धों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छोटे शहरों का
आर्थिक स्तर समान नहीं होता। धन का असमान वितरण अनेक तरह की सामाजिक समस्याएं
उत्पन्न करता है। आर्थिक रूप से पिछडे़ समाज में अनेक पारस्परिक अवरोध पाए जाते
हैं। जैसे अशिक्षा, गरीबी, कुपोषण, तीव्र जनवृद्धि सामाजिक व्यवस्था में बदलाव बहुत कुछ आर्थिक
प्रगति पर आधारित होता है।
यह आर्थिक स्तर ही मनुष्य के सामाजिक व मानसिक विकास का आधार बनता है। आर्थिक
असमानता के कारण मानसिक विकास भी एक सा नहीं होता। छोटे शहरों की सबसे बड़ी विशेषता
यही है कि इसका सामाजिक तथा मानसिक विकास साथ - साथ नहीं हो पाता।
छोटे शहरों की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी सुदृढ़ नहीं होती। जनता में राजनैतिक
चेतना का अभाव होता है, जिसका लाभ चतुर राजनीतिक संगठन खूब उठाते हैं। सवेदनशील
मुद्दों को उभारकर जनता की भावनाओं का ग़लत इस्तेमाल स्वार्थान्ध राजनीति के लिए
उर्वर साबित होता है। यही कारण है कि छोटे शहरों में साम्प्रदायिक राजनीति
पर्याप्त सफल होती है। राजनैतिक जागरूकता के अभाव में क्षेत्र की प्रगति भी नहीं
हो पाती। यदि होती भी है तो वोटों की राजनीति के कारण असमान और असंतुलित ढंग से
होती है। सड़कें, बिजली और पानी के अलावा राजनीति के पास कोई बडा लक्ष्य नहीं
होता। लक्ष्य और दिशा के अभाव में राजनीति भ्रमित होती है। यही कारण है कि छोटे
शहरों का लीडर दल के उसूलों व नियम - कायदों अथवा वैचारिक पृष्ठभूमि से अपरिचित
होने के कारण कभी - कभी विरोधी व्यवहार कर बैठता है। राजनीति को जनसेवा का माध्यम
न मानकर एक पेशे अथवा व्यवसाय से जोड़ा जाता है। व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति तथा
निजी हित को ही केन्द्र में रखने के कारण राजनीति लक्ष्यहीन रहती है।
धर्म समस्त पूर्वी एशियाई देशों के लिए रीढ़ के समान है। छोटे शहरों में धर्म
का स्वरूप बहुत हद तक अंधविश्वास और बाह्याचारों की सीमा को स्पर्श करता रहता है।
बाह्याचारों को ही सब कुछ मानने के कारण जनता धर्म के वास्तविक लक्ष्य से दूर ही रहती है। यही कारण
है कि धर्म के नाम पर राजनैतिक संगठन जनता का भरपूर शोषण करते हैं और उन्हें आपस
में टकराव के लिए उकसाते रहते हैं। छोटे शहरों में धर्म अधिकतर यथास्थितिवाद को ही
पोषित करता है। यदि किसी समाज में भ्रष्टाचार,
शोषण और अनाचार बढ़ता है तो बहुत सरलीकृत रूप में भौतिकवाद
को दोषी कहकर धर्म को बचा लिया जाता है। धर्म किसी भी प्रकार के अन्याय अथवा
अत्याचार के विरोध में खड़े होने के लिए व्यक्ति को अत्मबल नहीं प्रदान करता बल्कि
भाग्य का खेल और नियति का लेखा मानकार सब - कुछ निर्विरोधी रूप से सह जाने को
प्रेरित करता है। विभिन्न प्रकार की रूढ़ियां और धर्मभीरुता व्यक्ति को उग्र,
संशयग्रस्त और अनुदार बना देती हैं।
छोटे शहरों का वैचारिक परिवेश ‘विरूद्धों का सामंजस्य’
होता है। एक ओर तो विचारशीलता और स्वतंत्र चिन्तन के लिए
छोटे शहरों का परिवेश सर्वाधिक अनुकूल ठहरता है तो दूसरी ओर विचारहीनता के उपादान
भी उसी तीव्रता के साथ सक्रिय रहते हैं। चूँकि इन जगहों पर पारस्परिक प्रतिस्पर्धा,
राजनैतिक या संस्थागत दबाव,
तनावपूर्ण जीवन की परिस्थितियाँ,
एकाकी, जीवन की दिक्कतें आदि नहीं होतीं,
अतः विचारशील मस्तिष्क स्वतंत्र रूप से चिंतन कर सकने में
समर्थ होता है। जबकि दूसरी ओर बाजारवादी - उपभोक्तावादी समाज व्यक्ति की वैचारिकता
को सोख लेने को आतुर रहता है। यद्यपि महानगरों की भाँति विज्ञापनी चकाचौंध यहाँ
इतनी अधिक नहीं होती, पर उसका प्रभाव अत्यंत तीव्र होता है और व्यक्ति के जीवन को
बुरी तरह प्रभावित करता है। विविध तकनीकों ने हमारे दैनिक जीवन की विधियों को बहुत
अधिक प्रभावित किया है। हमारी जीवन शैली और हमारे सामाजिक सम्बध आकाशीय चैनलों की
प्रतिस्पर्धा में बुरी तरह फंस गए हैं। देसी-विदेशी चैनलों से पसरती अपसंस्कृति और
आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में हमारी सभ्यता-संस्कृति और परम्पराओं के साथ - साथ
सामाजिक व्यवस्था एवं मूल्य बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं।
ऐसी परिस्थितियों में सर्वाधिक प्रभावित साहित्य व रचनाकर्म होता है।
उपभोक्तावाद का साहित्य पर सबसे घातक असर तो यह है कि लोग उसके प्रति उदासीन हो
रहे हैं। टेलीवीज़न और विदेशी चैनलों ने लोगों का सारा समय ले लिया है। लोग साहित्य
के प्रति उदासीन नहीं हो रहे बल्कि सनसनीख़ेज,
उत्तेजक और सस्ते साहित्य की मांग बढ़ रही है। इसके साथ ही
लेखकों के सामने नए तरह के संकट खडे़ हो रहे हैं। उपभोक्तावाद लेखक की चेतना पर भी
जाने - अनजाने प्रभाव डालता है। विज्ञापन,
प्रलोभन और प्रचारवादी शक्तियाँ भी उस पर दवाव डालती हैं।
यह अकारण ही नहीं है कि अपने समय के हिन्दी के महत्वर्पूण कवि - कहानीकार इस
उपभोक्तावाद के खिंचाव में आकर टेलीवीज़न संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं,
सीरियलों में संवाद लिख रहे हैं और टेलीविज़न की मांग के
अनुसार सीरियल बनाने वालों का साथ दे रहे हैं।
यही समस्याएं छोटे शहर के लेखक, पाठक, दर्शक आदि के सम्मुख भी रहती हैं। छोटे शहरों के रंगमंच की
प्रमुख समस्या विचारशील दर्शकों का अभाव है। दर्शक रंगमंच की सबसे आवश्यक कड़ी होते
हैं। उनकी उपेक्षा या अभाव से रंगमंच का सफल होना संभव नहीं। रंगमंच की सफलता
सिर्फ दर्शकों पर निर्भर है। अतः दर्शक ही रंगमंच का मुख्य लक्ष्य होता है। किन्तु
छोटे शहरों के दर्शक वर्ग की अपनी कुछ समस्याएं होती हैं। उनमें वैचारिकता का अभाव
होता है। अतः उनकी पसंद हल्के - फुल्के मनोरंजक नाटक ही होते हैं। शाहजहाँपुर में
चूंकि रंगमंच की लम्बी और समृद्ध परम्परा रही है, अतः दर्शकों में रंगमंच की एक
सामान्य समझ अवश्य है, फिर भी हमारा समय जिस वैचारिक चेतना की मांग करता है। उसका
उनमें अभाव ही कहा जाएगा। यहाँ दर्शकों के दो वर्ग संतुष्ट हैं - एक प्रबुद्ध वर्ग,
दूसरा बिल्कुल नया दर्शक,
जिसे रंगमंच की बिलकुल समझ नहीं है। दूसरी ओर प्रबुद्ध वर्ग
रंगमंच की समझ के बावजूद विचारशील नाटक देखना नहीं पसंद करता। यही कारण है कि हल्के - फुल्के हास्य नाटकों का ही बोलबाला
है। विचारशील दर्शकों के अभाव के कारण ही कभी - कभी लचर प्रस्तुतियाँ सामने आ जाती
हैं।
दर्शकों का यह भाव ही रंगमंच के विकास और उत्साहवर्द्धन के लिए प्रगति की राह
बाधित करता है। किसी न किसी रूप में यह आर्थिक समस्याएं उत्पन्न करता है। मराठी
दर्शकों की भाँति यहाँ का दर्शक टिकट लेकर या सहयोग राशि देकर किसी भी रूप में
नाटक देखना नहीं चाहता। अतः रंगकर्मियों का न तो उत्साहवर्द्धन हो पाता है और न ही
साधनों की अल्पता का सवाल हल हो पाता है।
दर्शकों के अतिरिक्त रंगकर्मी भी मानसिक रूप से पूर्ण परिपक्व नहीं होते।
उनमें वैचारिक चेतना और प्रतिबद्धता का अभाव होता है। यहाँ का अभिनेता ‘हीरोइक’ छवि की रोमानियत लेकर मंच पर आता है। उसके ऊपर फिल्मों का
प्रभाव होता है। मंच पर अभिनय करके वह अपनी नायकीय मनोवृत्ति को संतुष्ट करना
चाहता है। टीवी चैनलों व फिल्मों में बढ़ते हुए अवसरों को देखकर वह रंगमंच को पेशे
के रूप में अपनाना चाहता है। जनपद के कुछ सफल रंगकर्मी उसके सामने आदर्श होते हैं।
अतः यहाँ का अभिनेता रोमानियत और व्यवसायिकता के बीच झूलता रहता है। इस परिवेश में
प्रतिबद्धता अथवा ‘प्रतिरोध के रंगमंच’
की बात करना बेमानी-सा हो जाता है। न तो अभिनेता के पास और
न ही निर्देशक के पास एक सुव्यवस्थित लक्ष्य होता है। नाटक करने के लिए ही नाटक
किए जाते हैं। यश प्राप्ति और बुद्धिजीवी कहलाने का लोभ वास्तविक लक्ष्य-प्राप्ति
में सबसे बड़ी बाधा होता है। महानगरीय रंगकर्मियों की तरह यद्यपि यहाँ का रंगकर्मी
उतना ‘प्रोफेशनल’ नहीं होता; उसमें सर्मपण एवं निष्ठा का भाव होता है। उसके बावजूद उस पर
रोमानियत का इतना ज्यादा प्रभाव होता है कि वह अपने समर्पण और निष्ठा का सदिश
उपयोग नहीं कर पाता।
इन समस्याओं के बावजूद यहाँ रंगकर्म के लक्ष्यपूर्ण विकास की पूरी सम्भावनाएं
मौजूद हैं। रंगकर्म को एक सामाजिक कर्म बनाने के लिए जिन बुनियादी तत्वों -समर्पण
एवं निष्ठा- की आवश्यकता होती हैं, यहाँ के रगंकर्मियों में यह पहले से विद्यमान होती है।
आवश्यकता सिर्फ उन्हें दिशा देने की होती हैं। लातीनी अमेरिका देशों ने प्रतिरोध
के साहित्य की जो अलख जगाई थी, रंगमंच के क्षेत्र में उसका सही अनुप्रयोग कस्बों और छोटे
शहरों में ही संभव है। शाहजहाँपुर का रंगमंच भी इस दृष्टि से कुछ अर्थो में सफल
कहा जा सकता है। सफदर हाशमी की हत्या के पश्चात् सुधीर विद्यार्थी के नेतृत्व में
व्यवस्था के विरोध में पूरे जनपद में ‘जागो-जागो-जागो’ शीर्षक से खेले गए और सफल रहे नुक्कड़ नाटक इस बात का
प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त वर्ण - व्यवस्था के विरोध पर आधारित ‘घर वापसी’, ‘हवन कुंड’ (निर्देशक-राजेश कुमार),
साम्प्रदायिक विरोध पर आधारित ‘अयोध्या’, ‘गांधी ने कहा था’ (निर्देशक-राजेश कुमार),
भक्तिकाल व रैदास के जीवन के ऐतिहासिक विश्लेषण के बहाने
सामाजिक विसंगति को उभारता ‘कह रैदास खलास चमारा’
(निर्देशक-राजेश कुमार) तथा
भ्रष्टाचार को बेनकाब करता ‘एक अधिकारी की मौत’
(निर्देशक-चन्द्रमोहन ‘महेन्द्रू’) आदि नाटक भी एक आशा बँधाते हैं।
महिला कलाकारों की कमी यहाँ की प्रमुख समस्या है। छोटे शहरों की सामाजिक-धार्मिक
परिस्थितियों का प्रभाव यहाँ की महिलाओं पर भी है। आमजन में नाटक की छवि आज भी एक
कला के रूप में न होकर लक्ष्यहीन और बेरोजगार युवाओं की निरूद्देश्य कर्म के रूप
में है। इसके अतिरिक्त रूढ़िवादी कस्बाई सोच भी इस मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है।
मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण पर्दाप्रथा आदि की धार्मिक रूढ़ियाँ भी इस
क्षेत्र की बड़ी बाधाएँ हैं। एक अन्य कारण यह भी है कि रंगमंच एक लम्बी प्रक्रिया
है। दर्शकों के सामने आने से पूर्व नाटक में गहन पूर्वाभ्यास और अत्यधिक समय की
आवश्यकता पड़ती है। अतः क्रिया की तुरंत प्रतिक्रिया चाहने वाला समाज रंगमंच से अपना
बहुत जुड़ाव नहीं महसूस कर पाता। महिला कलाकारों के लिए तो यह बहुत बड़ी बाधा बनता
है। यही कारण है कि रूढ़िवादी परिवारों के अभिभावक भी महिला कलाकारों को गायन और
नृत्य में प्रतिभाग करने को आज्ञा दे देते हैं,
पर रंगकर्म में नहीं। जनपद में आधुनिक नाटकों का आरंभ करने
वाली संस्था ‘अनामिका’ के उत्थान ने महिला कलाकारों को प्रोत्साहित किया था,
किंतु किन्हीं कारणोंवश ‘अनामिका’ के बाद यह निरन्तरता बनी न रह सकी । किंतु इसके बावजूद जनपद
के रंगमंच पर कुछ ऐसे नाम उभर कर सामने आते हैं जो स्थिति को पूरी तरह से
निराशाजनक नहीं होने देते। गुलिस्तां, बबिता पाण्डेय (दोनों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में चयनित),
शोभा डे, शाज़ली, शैफाली, आरती, प्रिया, शालू आदि का नाम इसी क्रम में लिया जा सकता है।
संसाधनों की अल्पता तथा आर्थिक कमजोरी बहुत बड़ी समस्या है जो न केवल रंगकर्म
की सक्रियता को प्रभावित करती है, बल्कि उसके स्तर को भी जाने अनजाने प्रभावित करती है।
पूर्वाभ्यास, मंच-सज्जा, रूप-सज्जा, ध्वनि-प्रकाश आदि ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनमें पर्याप्त धन की
आवश्यकता होती है। हजारों के खर्चें बिना किसी संस्था या सरकार के सहयोग के पूरे
हो सकने संभव नहीं होते। इस क्षेत्र में सरकारी सहयोग शून्य है। शासन के
उपेक्षापूर्ण व्यवहार से रंगमंच विकसित नहीं हो पा रहा। प्रेक्षागृह के लगातार
बढ़ते किराये ने समस्या को और पेचीदा किया है। दर्शक टिकट खरीदने के लिए तैयार नहीं
होता क्योंकि मध्यवर्गीय पेचीदगियों से ऊब कर दर्शक जिस फैंण्टेसी में जाने के लिए
आता है। उसमें वह गम्भीर और विचारशील नाटक भी नहीं देखना चाहता। रंगकर्मियों को
कभी-कभी राजनेताओं और शासन का अनुदानात्मक सहयोग लेना पड़ जाता है। इससे नाटकों की
प्रतिबद्धता के लिए संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है। वे चाहकर भी व्यवस्था का
विरोध नहीं पर पाते और यथास्थिति की स्तुति में ही उनका पर्यावसान हो जाता है।
आर्थिक साधनों की पूर्ति का सबसे प्रमुख साधन विज्ञापनों द्वारा प्राप्त आय है,
किंतु कभी-कभी विज्ञापनों का सहारा लेना अन्तर्विरोधात्मक
स्थितियां उत्पन्न कर देता है। राजेश कुमार द्वारा लिखित व निर्देशित ‘मुगलों ने सल्तनत बख़्श दी’
नामक एकल पर यह आरोप लगाया गया कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों
के फैलते हुए जाल का विरोध करने के बावजूद रंगकर्मियो ने प्रचार व प्रदर्शन में
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की क्षेत्रीय शाखाओं से सहायता ली। किंतु इन जटिल समस्याओं
के बावजूद यहाँ का रंगमंच अपने उद्देश्य और अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को बचाए रखने
में सफल रहा है।
नाटक की अंतिम परिणति मंच पर दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत होना है। किंतु इससे
पूर्व उसे तमाम लम्बी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। इन प्रक्रियाओं की सफलता पर
ही नाटक की मंचीय सफलता तय होती है। सहज, स्वाभाविक और यथार्थ प्रदर्शन के लिए तथा ‘रीटेक’ की सम्भावनाओं के न होने के कारण नाटकों को गहन पूर्वाभ्यास
की आवश्यकता होती है, पूर्वाभ्यास के लिए एक निश्चित और उपयुक्त स्थान अत्यंत
आवश्यक है। जहाँ स्थाई रूप से विभिन्न साधन जुटाए जा सकें। जनपद के नाटककारों के
सम्मुख सबसे बड़ी समस्या उपयुक्त पूर्वाभ्यास स्थल की है। यहाँ के रंगकर्मी विभिन्न
स्कूलों में पूर्वाभ्यास करते हैं। अभिव्यक्ति संस्था एस.पी.कॉलेज में,
विमर्श एस.पी.कॉलेज की नई विल्डिंग में तथा अन्य संस्थाएं
भी इसी प्रकार विद्यालयों को आश्रय स्थल बनाएं हुए हैं।
रंग प्रदर्शन के उपयुक्त प्रेक्षागृह का अभाव मंचन की प्रमुख समस्या है।
स्थानीय गांधी भवन नाट्य प्रर्दशन हेतु विशेष रूप से तैयार नहीं किया गया है। अतः
नाट्य प्रदर्शन के दौरान उपयुक्त ‘इन्फ्रा स्ट्रक्चर’
का अभाव रंगकर्मियों के लिए एक गहरी समस्या है। वातानुकूलित
कक्ष न होने कारण प्रेक्षागृह के दरवाजे़ खुले रहते हैं। अतः बाहर की हलचलें और
ध्वनियां नाट्य प्रदर्शन को बाधित करती हैं। अभिनेताओं के संवाद तथा ध्वनि का
प्रभाव भी उतना सशक्त नहीं हो पाता है। अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था,
डिमर का कार्य न करना,
स्पॉट लाइटों का खराब होना तथा ध्वनि व्यवस्था के लिए
उपयुक्त संरचनाएं न होना नाट्य प्रदर्शन में बड़ी बाधा उपस्थित करता है। कभी-कभी
प्रेक्षागृह का दूसरे कार्यो में इस्तेमाल रंगकर्मियों को हतोत्साहित करने वाला
होता है। गांधी भवन को बारात घर बनाए जाने पर रंगकर्मियों ने गहरी आपत्ति दर्ज की
थी। इसके अतिरिक्त प्रेक्षागृह का अधिक किराया रही-सही कसर पूरी कर देता है।
रंगकर्मियों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा,
व्यक्तिगत स्वार्थ तथा यश प्राप्ति का लोभ रंगकर्म के
स्वस्थ विकास में गहरी बाधा उत्पन्न करता है। प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ के कारण
रंगकमिर्यो में पारस्परिक द्वन्द्व पनपता है तथा संस्थाओं में बिखराव और टूट होती
रहती है। सारी प्रसिद्धि स्वयं प्राप्त करने का लोभ नई-नई संस्थाओं को जन्म देता
है। वर्तमान समय में जनपद में दर्जन से अधिक रंग संस्थाएं हैं। कुछ संस्थाएं तो
ऐसी हैं। जिन्होंने एक या दो नाटक करके अपना नाम रंगमंच के इतिहास में दर्ज कराने
की अपेक्षा रखती हैं। इससे नाटकों की गुणवता तो प्रभावित होती ही है साथ ही रंगमंच
की सोद्देश्यता और प्रतिबद्धता पर भी असर पड़ता है। युवा वर्ग भी लक्ष्यहीन होकर
भटकता है। जनपद के वरिष्ठ रंगकर्मियों का विचार है कि एकजुटता न होने से दर्शकों में
उदासीनता आती है। एकजुटता से हमारे स्तर में सुधार होता है और दर्शक जागरूक होता
है। वरिष्ठ रंगकमिर्यों को यह भी शिकायत है कि नए रंगकर्मियों में सीखने का उत्साह
तो है पर उनमें समर्पण का भाव नहीं है। कम परिश्रम में वे अधिक सफलता चाहते हैं।
अपने से बड़ों के प्रति उनमें सम्मान का भाव नहीं है। अहं को त्यागकर वे निःस्वार्थ
भाव से रंगकर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होते। यही कारण है कि गुटबन्दी बढ़ती है और
नई-नई रंग संस्थाएं कुकुरमुत्तों के समान उग आती हैं।
जबकि दूसरी ओर नए रंगकर्मी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। उनके अनुसार
वरिष्ठ रंगकर्मियों का अहंवादी रवैया ही उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने को
विवश करता है। नवीन सूचनाओं और परिवर्तित परिवेश से सामंजस्य न बिठा पाने के कारण
वरिष्ठ रंगकर्मी लीक पीटने में लगे रहते हैं। इस कारण वे न तो नबागन्तुक
रंगकर्मियों की प्रतिभा का सही उपयोग कर पाते हैं और न ही कुछ सिखा पाते हैं।
उनमें गुरु-शिष्य की जड़ परम्परा का बोध सदैव जाग्रत रहता है। इससे दोनो के बीच एक
गैप आ जाता है। यह गैप ही गुटबन्दियों और नई-नई संस्थाओं के जन्म का कारण है।
जबकि कुछ रंगकर्मी अपेक्षाकृत वैज्ञानिक ढ़ंग से सोचते हैं। उनके अनुसार वरिष्ठ
और कनिष्ठ रंगकर्मियों के बीच आए गैप के लिए कोई एक वर्ग दोषी नहीं है। यह कमियां
दोनो वर्गों को दूर करनी होंगी। दोनों को एक-दूसरे के करीब आना होगा,
यह गैप तभी भर सकेगा। इसके साथ-साथ एक रंगमंच एसोसियेशन का
निर्माण होना चाहिए, जहाँ प्रतिमाह होने वाली बैठकों में हर व्यक्ति अपनी
अभिव्यक्ति कर सके।
रंग-प्रशिक्षण का अभाव भी छोटे-शहरों के रंगमंच को प्रभावित करता है। जनपद में
न तो कोई प्रशिक्षण संस्थाए हैं और न ही अनुभवी प्रशिक्षक। अतः यहाँ का रंगकर्मी
स्वतः स्वानुभवों से सीखता है। यद्यपि बीच में रंग कार्यशालाएं आयोजित की जाती रही
हैं। किन्तु ये प्रयास अल्प ही कहे जाएंगे। आधुनिक नाटकों की शुरुआत जब अनामिका ने
की तो रंग-कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। भारतेन्दु नाट्य अकादमी के अनुभवी
रंगकर्मियों ने प्रशिक्षण दिया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और भारतेन्दु नाट्य
अकादमी में चयनित छात्र भी वापस आकर कार्यशालाएं लगाते हैं। बबिता पाण्डे,
राजपाल यादव, गुलिस्तां, मोअज़्ज़म बेग, तौकीर वारसी आदि यहाँ नाट्य कार्यशालाएं आयोजित कर चुके
हैं।
उपर्युक्त के अतिरिक्त कभी-कभी धार्मिक-सामाजिक रूढ़ियां भी बाधा उत्पन्न करती हैं।
‘एक था गधा उर्फ अलादाद खाँ’ के मंचन पर वर्ग विशेष के लोगों की आपत्ति के कारण ही इसका
शीर्षक परिवर्तित करके ‘एक था गधा’ कर दिया गया था। मुअज़्ज़म बेग के प्रयोगवादी नाटक ‘कमबख़्त इश्क’ में चित्रगुप्त पर किए गए कटाक्ष को लेकर एक वर्ग रुष्ट हो
गया था, जिसके कारण इसका मंचन काफी समय तक लंम्बित रहा। अक्सर कहा
जाता है कि छोटे शहर का रंगमंच छोटा होता है,
यह बात पूरी तरह से सटीक नहीं बैठती,
क्योंकि छोटे-बडे़ का फर्क रंगमंच के उद्देश को लेकर होना
चाहिए न कि शहर को लेकर। उपर्युक्त विवेचन पर यदि ध्यान दे तो शाहजहाँपुर एक छोटा
शहर है और इस कारण यहाँ के रंगकर्मियों के समक्ष सामाजिक,
धार्मिक, आर्थिक आदि तमाम सारी समस्याएं उपस्थित हैं,
पर इस आधार पर इसको छोटा कहना संगत न होगा। शहर का छोटा
होना अर्थात् आवश्यकताओं का अभाव ही शाहजहाँपुर रंगमंच को बड़ा बना देता है,
क्योंकि छोटे शहर के रंगकर्मियों में नाटक के प्रति जो
वैचारिक, सामाजिक प्रतिबद्धता है,
वह बड़े महानगर के रंगकर्मियों में कम दिखती है। लखनऊ,
भोपाल या दिल्ली के रंगकर्मियों पर दृष्टि डालें तो आप
पाएंगे कि वे खुद को अधिक ‘प्रोफेशनल’ बताते नहीं थकते। ‘प्रोफेशनल’ शब्द उस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं कि उनके अभिनय की कीमत
अगर कोई संस्था अदा करने की स्थिति में हो तो उनका उपयोग कर सकती है। ऐसे ‘प्रोफेशनल’ कलाकारों का नाटक की विचारधारा से कोई सरोकार नहीं होता। पर
छोटे शहर से जो रंगकर्मी आते हैं उनका मकसद पैसा कमाना कभी नहीं होता। वे नाटक के
माध्यम से कहीं न कहीं अपने आप को समाज से जोड़ते हैं। शाहजहाँपुर रंगमंच पर भी ऐसे
कलाकारों की कमी नहीं है। यहाँ बहुत से ऐसे कलाकार आपको मिल जाएंगे जो होटल पर
रोटियां सेकते हैं, साइकिल के पंक्चर जोड़ते हैं,
कबाड़ की खरीद-फरोख़्त करते हैं,
गलियों-मोहल्लों में घूम-घूमकर कुकर आदि की रिपेयरिंग करते
हैं लेकिन रंगमंच से पूरी तत्परता के साथ जुड़े हैं।
शाहजहाँपुर के रंगमंच से रूबरू होते हुए तमाम ऐसे रंगकर्मी नजर आते हैं,
जो ‘प्रोफेशनलिज्म’ का क ख ग भी नहीं जानते। अब चाहे वह ‘कह रैदास ...’ का रैदास हो , मटकाराम हो या कोई अन्य। यही कारण है कि बडे शहरों के ‘प्रोफेशनलिज्म’ के चक्कर में वहाँ का थियेटर ‘हास्य कवि सम्मेलन’
या ‘लाफ्टर शो’ बनता जा रहा है, जबकि छोटे शहर का रंगमंच कलात्मक स्तर पर मजबूत दिखाई देता
है।
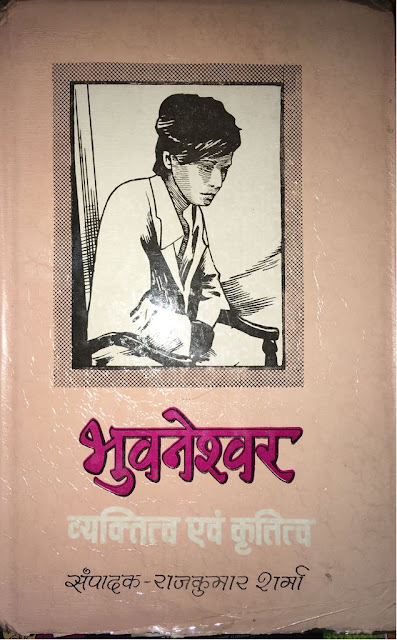
Comments
Post a Comment