जो बीत गईं वह बातें, संबल भरतीं जीवन में …
क्या बला का खूबसूरत था स्नातक से लेकर शोध तक का समय । एक अलग ही जुनून हुआ करता था पढ़ने का । नहाना, खाना, जीवन की दिनचर्या जैसे शब्दों का कोई महत्त्व ही न हुआ करता था । जितना पढ़ता जाता, अज्ञानता का दायरा उतना ही बढ़ता जाता । लेकिन क्या ही गज़ब का जुनून हुआ करता था । अध्यापकों और साथी लड़कियों के मन में बसने का लालच । विद्वान बनने की अति महत्त्वाकांक्षा । साथियों के बीच श्रेष्ठता का दंभ । बहुत कुछ दिखावटी सा हुआ होगा, आज दिखता है । बावजूद इसके पढ़ने लिखने की ललक मज़बूत से मज़बूत होती गई । स्नातक से लेकर आगे तक, सिलेबस तो कभी पढ़ा ही नहीं । बस उससे जुड़ी सैकडों किताबें चाटता रहता । बाबा कहते "असल पढ़ाई तो सिलेबस के बाहर की ही होती है ।" … और जब पढ़ने में मन न लगता या कुछ समझ में न आता तो बापू समझाते "किताब को आँखों के सामने से हटने न दो, कितनी देर समझ में न आएगी । पढ़ते जाओ, बस पढ़ते ही जाओ ।" साथी ही अलग-अलग प्रकार की किताबें सुझाते । … आगे चलकर अरशद और साजिद सर ने तो जैसे भूचाल ही ला दिया जीवन में । वो मेरे जीवन के आदर्श बनकर आए । लेखन के साथ जीने वाले इन दोनों आदर्शों ने किताबों की एक नवीन दुनिया स्थापित की मेरे सामने । मुझे खूब याद है । स्नातक का अंतिम वर्ष । जिसमें 'पालि' भाषा पढ़नी थी । एक छोटी सी पुस्तिका लगी थी पाठ्यक्रम में । कुंजी टाइप की । मुझे रास न आई । मैंने अरशद सर को बताया । वो भी खूब जुनूनी । पुस्तकालय से भरतसिंह उपाध्याय की एक किताब खोज लाए । तकरीबन 700 पेज की । मैंने एक सप्ताह में पढ़ डाली । साथ ही ऐसे नोट्स भी बना लिए जो सिविल की तैयारी करने वालों के लिए सर ने प्रेरित किए । एक बार जून के महीने की छुट्टियों में जब अनिल घर चले गए और मुद्गल जी अपने बेटों के पास दिल्ली । पूरे घर मे अकेला ही रह गया था । इस समय मैंने रूसी साहित्य की 50-60 किताबें मंगबाई थीं । धीरे धीरे पढ़ भी रहा था । अचानक न जाने ऐसा खुमार छा गया कि करीब 23 दिन तक घर का दरबाजा न खोला । ब्रेड और मैंगी के अलाबा कुछ भी न खाया । सेविंग न की । नहाया नहीं । घर में झाड़ू तक न लगाया । बस पढ़ता रहा । सोता रहा । सोता रहा और पढ़ता रहा । पूरा रसियन साहित्य पढ़ गया । 23 दिन बाद जब अनिल गाँव से वापस आए तो घर का ताला खुला । मुद्गल जी वापस आने वाले थे तो दो दिन घर की सफाई चली । क्या दिन थे वो । सोचता हूँ तो आज की स्थिति देखकर कलेजा मुँह को आ जाता है ।
एम. ए. और उसके दो तीन साल बाद के दौरान शाहजहाँपुर में मुद्गगल बाबा के घर रहता था । उस समय मेरा कमरा कुछ ऐसा हुआ करता था । कपडे लित्ते कम और किताबें अधिक । तकिया किताबें, बिस्तर किताबें, बेड किताबें और दोस्त किताबें । वह ऐसा दौर था जब किताबें बातें किया करती थीं । नियमत: रोज ही एक किताब पढना हो ही जाता था । ऊपर से मुद्गल बाबा से पढने को लेकर प्रतिस्पर्धा । इस प्रतिस्पर्धा ने न जाने कितनी अच्छी किताबें पढा डालीं ।
अब कमाने-खाने के चक्कर में पड़ गया हूँ । व्यवस्थित पुस्तकालय है । करीने से सजी किताबें और पोस्टर कई बार रुआंसे से कह पड़ते हैं - "सुनील अब तुम वह नहीं रहे । तुम्हारी अंगुलियों का स्पर्श पाने को मन बेताब हो उठता है । अब तुम अधिक लिखने लगे हो । छपने लगे हो, लेकिन मुझे तुम उसी रूप में अधिक पसंद थे ।"
वास्तव में अब उस समय की अपेक्षा अधिक किताबें हैं लेकिन उतना पढ़ नहीं पाता हूँ । अलमारियों से मेरी ओर झांकती किताबों के अंदर जो कसक है, वह मेरे अंदर भी है ।
फिलहल अपने आप को वापस इकट्ठा कर रहा हूँ । सोच रहा हूँ कि वही ऊर्जा 'शब्द' में भी आए । और इसके लिए मुझे वापस किताबों की इस दुनिया में पागल बनकर आना होगा । तभी 'शब्द' के आस पास पढ़ने का वातावरण उत्पन्न होगा । वैसे अभी भी उसके आस पास वैसा वातावरण है ही लेकिन पर्याप्त नहीं है ।
सुनील मानव
04.10.2020



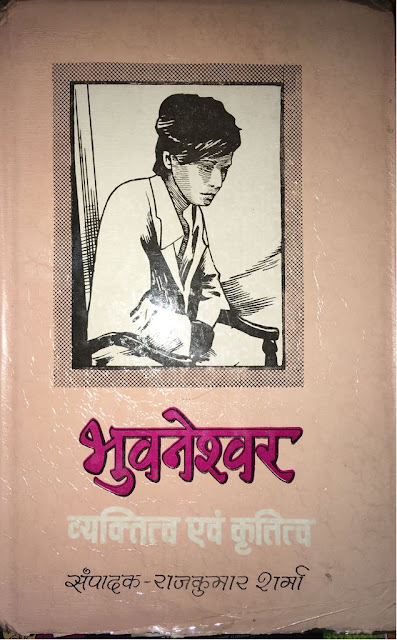
Comments
Post a Comment