साहित्य के बने बनाए ढ़ाँचे को अस्वीकारती ‘गंठी भंगिनियाँ’
पुस्तक : गंठी भंगिनिया
लेखक : सुनील मानव
विधा : कथा-पटकथा
प्रकाशक : अनुज्ञा बुक्स, नई दिल्ली
संस्करण : 2019 (प्रथम)
मूल्य : रु. 200 (हार्ड बाउंड)
‘गंठी भंगिनियाँ’ सुनील मानव नई कृति है जो साहित्य रूप के बने-बनाए ढ़ाँचे को अस्वीकारती है । अस्वीकार का कारण केवल नवीनता-प्रकाशन की आकाँक्षा नहीं है, बल्कि अपनी अनुभूतियों को प्रमाणिक रूप में व्यक्त करने की चेष्टा भी है ।कई बार साहित्य-रूप के आग्रह के कारण अनुभूतियों को अपने वास्तविक रूप से हमें लेखन के दौरान अलग करना पड़ता है । लेखक का ध्यान मुख्य रूप से इसी बिन्दु पर केन्द्रित था । अत: पूर्व निर्धारित ढ़ाँचे से इसमें अन्तर आना स्वाभाविक भी था और आवश्यक भी । यह कहना लाज़मी है कि यदि यह पुस्तक केवल पटकथा, कथा, संस्मरण और रिपोर्ताज के रूप में होती तो निश्चय ही अपनी प्रभावान्विति का बहुलांश खो देती और एक विशेष प्रकार की कृत्रिमता इस पर हावी हो जाती । लेखक ने रचना को उससे बचाया है जिसे चाहे तो लेखक की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि कह सकते हैं । लेखक, लेखक होने की अह्मन्यता से मुक्त है । उसे अपनी सीमाओं का ध्यान भी है । स्वयं उसी के शब्दों में “मज़बूरी यह कि मैं अधिक कल्पना नहीं कर पाता, इसलिए जो जिया उसी को ले लिया । अनगढ़ता बहुत है । इसलिए इसे लेखकीय कृति न माना जाए । अभी लेखक नहीं बन पाया हूँ । बन जाऊँगा तब की तब देखी जायेगी ।” यह स्वीकारोक्ति आकस्मिक या कृत्रिम नहीं है, वरन् लेखक की ईमानदारी का उद्घोष है ।
पुस्तक में संवाद को छोटे-छोटे वाक्यों में संयोजित किया गया है जिससे अभिप्रेत तथ्य अपनी पूरी स्पष्टता के साथ व्यक्त हुआ है । लम्बे-लम्बे वाक्यों में कई बार अभिव्यक्ति उलझकर रह जाती है और यह उलझाव भी बहुधा मानसिक होता है । प्रस्तोता स्वयं कई बार अनिर्णय की स्थिति में होता है कि वास्तव में उसे कहना क्या है ? अत: उलझे हुए शब्दों अथवा वाक्यों का प्रयोग करता है । यह अलग बात है कि सचेत पाठक की दृष्टि ठीक ऐसे ही स्थलों पर जा टिकती है और तथ्य उजागर हो जाता है । छोटे-छोटे वाक्यों में अपेक्षाकृत अधिक स्पष्टता होती है । अत: भाषा की दृष्टि से उसे अधिक अभिव्यक्ति सक्षम कह सकते हैं । ऐसी भाषा के खतरे भी हैं क्योंकि वैशिष्ट्य एवं सीमाएँ यहाँ दोनों ही अनावृत्त रहती हैं । इसी तथ्य को ध्यान में रखकर मैंने लेखक के शब्दों को ईमानदारी का उद्घोष कहा है । उक्त संदर्भों में कहने को और अधिक तथ्य हैं; किन्तु उसके विस्तार में न जाकर पुस्तक की अंतर्वस्तु पर विचार करना अधिक समीचीन समझता हूँ ।
इस पुस्तक में जो समस्या उठाई गई है वह नवीन नहीं है । ज्योतिबा फ़ुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, प्रेमचन्द, हीरा डोम, मलखान सिंह, ओमप्रकाश वाल्मीकि, जय प्रकाश कर्दम, सुभाष गताड़े, तुलसीराम, शरण कुमार लिम्बाले, अद्वैत मल्ल वर्मन आदि की एक लम्बी सूची है, जिस पर विस्तार से चर्चा भी हुई है । नाटक और सिनेमा को प्रभावान्विति की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त विधा माना गया है, किन्तु नाटक एवं सिनेमा में हुई दलित अभिव्यक्तियों का विश्लेषण कम ही हुआ है ।
‘गंठी भंगिनियाँ’ में जाति-संघर्ष एक ग्रामीण स्तर पर उठाया गया है जिसमें एक वर्ग (ब्राह्मण) अपने जातीय गर्व में इतना मतान्ध है कि दूसरे को अछूत समझना और उसे शिषित कर हाशिये पर डालना स्वाभाविक समझता है, तो दूसरा वर्ग (मेहतर), जिसका प्रतिनिधित्व ‘गंठी भंगिनियाँ’ करती है, जिसमें सदियों से शोषित उत्पीडित होने के कारण मुक्ति की आकांक्षा भी ठीक से पनप नहीं पायी थी और ‘सब कुछ नियति का खेल है’ मानकर यथास्थिति को बनाए रखने में अपना योगदान दे रही थी । यह समस्या किसी गाँव विशेष की होती हुई भी उतनी ही वैश्विक है जितनी कि क्षेत्रीय या ग्रामीण । लोक जीवन में मुक्तिकामी जीवन-मूल्य एवं प्रतिगामी जीवन-मूल्य दोनों ही विद्यमान होते हैं । इसका उदाहरण ‘परकास’ नामक पात्र है । जहाँ एक ओर जाति-भेद एवं छुआछूत की भावना की जड़ें गहरे पैठी हैं वहीं सवर्ण के बीच यह मान्यता भी है कि ‘भंगी’ के स्पर्श से श्वेत कुष्ठ नामक रोग ठीक हो जाता है । प्रगतिशील मूल्य एवं प्रतिगामी जीवन जीवन मूल्य दोनों के ही उदाहरण यहाँ एक साथ मिल जाते हैं । ‘भंगी’ का स्पर्श जहाँ रोग के बहाने ही सही उचित ठहराया गया है प्रगतिशील मूल्य का कार्य करता है । यदि स्पर्श का यह भाव स्पर्श-भावना से ऊपर उठकर सामान्य स्तर पर आ जाये तो मुक्ति के पथ पर एक क्रांतिकारी कदम होगा, किन्तु जड़ीभूत एवं स्वार्थप्रेरित भावना सवर्ण को इस स्तर तक आने नहीं देती । यह प्रतिगामी जीवन-मूल्य निरन्तर अभ्यास के कारण संस्कार में परिणत हो गया है । इस पुस्तक की एक और बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कुछ भी बाह्यारोपित नहीं है ।
लेखक ने जैसा देखा-समझा है अपने कौशल के साथ यथावत् प्रस्तुत कर दिया है । अपनी ओर से कोई उपदेश या आग्रह के बिना । इस फ़ैशन ने समाज और साहित्य का बड़ा नुक्सान किय आहै जिसमें लेखक प्राध्यापकीय भूमिका में आकर सामाजिक नियामक तय करने लगता है और पाठक को छात्र मान लेता है । जबकि शिक्षा-जगत को नई दृष्टि एवं विजन प्रदान करने वाले, बल्कि दिशा बदल देने वाले ख्यातिलब्ध शिक्षाशात्री जॉन हॉलर का मानना है कि हम किसी को कुछ सिखा नहीं सकते । वास्तव में किसी विषय के बारे में हम अपने अनुभव को साझा करते हैं और बहुदा वह दूसरे के अनुभव से मेल खा जाता है, किन्तु सं भावना इसकी भी पर्याप्त बनी रहती है कि दूसरे का अनुभव कुछ भिन्न और कई बार यह विपरीत भी हो सकता है । यही कारण है - ‘गंठी भंगिनियाँ’ संघर्ष के नए-नए उपकरणों की खोज करती नहीं दिखाई देती । बदलते परिवेश एवं बदलती हुई सामूहिक चेतना के साथ-साथ उसकी स्थिति भी बदलती जाती है ।
वास्तव में सामाजिक विकास की प्रक्रिया एक रेखीय प्रणाली का अनुगमन नहीं करती, कम से कम आज के समाज में तो बिलकुल नहीं । जहाँ ‘कआस थियरी’ (अव्यवस्था का सिद्धांत) एवं ‘पोस्ट ट्रुथ थियरी’ की सीमाएँ भी स्पष्ट होने लगी है । यदि विकास की ऐतिहासिक प्रक्रिया को ही देखें तब भी उससे सहमत नहीं हुआ जा सकता । कई बार सहज-स्वाभाविक ढंग से परिस्थिति-प्रसूत चेतना भी सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है जिसमें विकास की प्रक्रिया तेज नहीं होती तो संघर्ष का मूल्य भी रक्तिम रूप में नहीं चुकाना पड़ता । ध्यातव्य है कि अपनी इसी विशेषता के कारण लेखक का वक्तव्य भी लेखक का वक्तव्य न होकर व्यापक समुदाय की चेतना के एक स्तर के रूप में व्यक्त होता है ।
यहाँ लेखक न तो अतीत जीवी है और न ही भविष्यद्रस्टा । अत: न तो पुस्तक में शोषण की प्राचीन प्रणाली एवं उपकरण की बात करता है और न ही मुक्ति-उपरान्त की स्वर्णिम निर्मितियाँ करता है । वह वर्तमान की यात्रा में है और वर्तमान में ही अपनी यात्रा पूरा करता है । यही कारण है कि कहीं भी संभावनाओं को कीलित नहीं किया है । जीवन निरन्तर प्रवाह है और इस प्रवाह में ही उसकी सीमाओं एवं उपलब्धियों से सामना होता है । यह तर्क यहाँ व्यर्थ जान पड़ता है जो कभी नई कविता के लिए दिया गया था कि ‘उनके पास न तो स्वर्णिम अतीत था जिस पर वे गर्व करते और न भविष्य की स्पष्ट रूपरेखा ही । कारण कि यहाँ लेखक कृतिकार है न कि सिद्धांतकार ।
कुल मिलाकर ‘गंठी भंगिनियाँ’ अपनी अनगढ़ता एवं शैल्पिक अभाव के बावजूद महत्त्वपूर्ण पुस्तक है जो समाज में व्याप्त रूढ़ियों एवं समाजगत व वर्गगत भेद से परिचित कराती है । साथ ही उन्हें लेखकों की जमात में शामिल होने का प्रमाण भी देती है ।
डॉ. राकेश कुमार सिंह

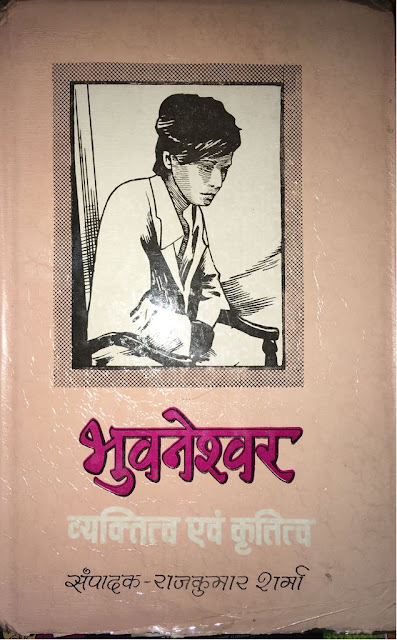
Comments
Post a Comment