खानबन्धु की बाल कविताओं के वैश्विक आयाम
आज के दौर में भी जब हम बालसाहित्य की बात करते हैं तो हमारे मनोमस्तिष्क में वह बाल छवि अनायास ही कौतूहल मचाने लगती है, जिससे हम निकलकर आए हैं अथवा जिसके संग-साथ हम रोज ही अपने बचपन को महसूस करते हैं। बच्चों की मासूमियत, उनकी संवेदना, उनके मनोभाव, उनके सहज से तर्क और प्रश्न हमें कभी-कभी निरुत्तर से कर देते हैं।
सुभद्रा जी की कविता की ‘बिटिया’ ज्यों ही अपने नन्हें हाथों में ली हुई मिट्टी को माँ की ओर खाने को बढ़ाती है, माँ का हृदय अह्लाद से भर उठता है। सुनील मानव की बाल लघुकथा ‘मैंने शू-शू कर ली’ एवं ‘मम्मी थक जाती हैं ना दादा’ का नन्हा नायक ‘शिखर’ अपने मासूमियत से भरे तर्कों से बड़े और गंभीर मस्तिष्कों को निरुत्तर कर देता है। कहने का तात्पर्य यह कि बालमन में तर्क-वितर्क नहीं केवल कोमल भाव निहित होते हैं। उन पर वातावरण का प्रभाव उनके बढ़ते जाने के साथ-साथ ही पड़ने लगता है।
आज का दौर बाज़ारवाद का दौर है। हमारे जीवन के समस्त पहलुओं को बाजार अपनी चपेट में लेता जा रहा है। हमारे जीवन की प्रत्येक आवश्यकता का निर्धारण बाजार ही कर रहा है। यहाँ तक कि बच्चों की सुकुमार संवेदना को भी ग्रहण लग रहा है। बच्चों के खेल-खिलौनों की दुनिया से कब गुड्डे-गुड़िया, बाजे-नगाड़े आदि निकलते चले गए और कब उनकी जगह ‘बंदूक’ जैसे खिलौनों ने ले ली पता ही नहीं चला। बाजारीकरण ने हमारे संस्कारों में कब विष उतार दिया, हमें आभाष ही न हुआ।
आज के समय में कम्प्यूटर बच्चों के आकर्षण का मुख्य नायक है। कम्प्यूटर ही बच्चों के खेल, शिक्षा और गुरु का स्थान लेता जा रहा है। बाल-कथाओं की पुस्तकों से बच्चे करीब-करीब अलग हो गये हैं। संयुक्त परिवार टूटकर एकल बनते जा रहे हैं। रिश्ते संकुचित हो रहे हैं। माँ-बाप ‘नौकरी’ करने के चक्कर में बच्चे से दूर हो रहे हैं। बच्चों का लालन-पालन ‘आयाओं’ द्वारा किया जा रहा है। दादी-नानी की कहानियाँ तो अब बीते जमाने की बात हो गई हैं। ऐसे में बच्चे पूरी तरह से मीडिया, टी.वी. और कम्प्यूटर पर निर्भर होते जा रहे हैं। कम्प्यूटर ही आज बच्चों का साथी और गुरु बनता जा रहा है। ‘हैरी पॉर्टर’ की अतिकाल्पनिक दुनिया और ‘स्टंटमैंन’ के सपनों से होड़ लगाती बच्चों की कल्पना अपनी जमीन से पृथक होती जा रही है। आधुनिक सुख-सुविधाओं से युक्त ‘मॉर्डन’ विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा के स्थान पर बड़ा-से-बड़ा ‘नौकर’ बनाने की होड़ लगी है।
कहने का तात्पर्य यह कि आज समय के साथ बच्चा आधुनिक होने लगा है। उसके तर्क बदल गए हैं, उसके खेल बदल गए हैं। पहले जहाँ बालक के नायक परियों की कथाओं के अतिकाल्पनिक दूसरी दुनियाँ के जीव होते थे, वहीं आज शक्तिमान, हैरी पॉर्टर, कृष आदि बच्चों के हीरो हो गए हैं। यह हीरों भले ही अति आधुनिक और अतिकाल्पनिक हों, लेकिन हैं तो उनकी ही दुनियाँ के, जिनको वह देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। उन्हें यह नहीं लगता कि जिनके बारे में वह सुन रहा है वह दूसरी दुनिया के हैं, वह भले ही स्क्रीन पर दिखते हैं, पर दिखते तो हैं ही। बच्चों को वह अपने आस-पास के लगते हैं।
आज का बालक सिनेमा और साइंस की दुनिया में जी रहा है। उसके हाथ में नया फोन है। कभी-कभी लगता है कि विज्ञान उसकी सहचरी बन गई हो, तो ऐसे बालक की कल्पना भी तो उसी कोटि की ही होगी ना। ऐसे बच्चे के लिए साहित्य की रचना करना महज मजाक थोड़े ही ना है। बड़ा ही दुस्साध्य कार्य है। बच्चे के संपूर्ण मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा भाई।
बालसाहित्य के सामने आज तमाम प्रश्न चीख-चीखकर उत्तर की माँग के नारे लगा रहे हैं।
आज कितने बच्चे हैं जो प्राचीन लोरियाँ सुनते हैं?
आज कितने बच्चे हैं जो प्राचीन अर्थात् हमारे बचपन के ही खेल खेलते हैं?
कितने बच्चे हैं जो पुराने तरीकों से लिखते-पढ़ते और सीखते हैं?
ऐसे में एक प्रश्न यह उठता है कि जब आज बच्चों के रहन-सहन से लेकर उनके खेलने-खाने, लिखने-पढ़ने और सोचने-समझने तक के तरीके बदल गए हैं तो फिर आज का बालसाहित्यकार किसके लिए और क्यों लिख रहा है?
क्या केवल प्रशंसा एवं प्रसिद्धि के लिए?
आज कोई पत्रिका में किसी लेखक का परिचय हो अथवा सोशल मीडिया पर स्वयं लेखक द्वारा अपनी प्रशंसा में दिया गया परिचय हो; सबमें दिखता है कि उक्त विद्वान ने इतना साहित्य लिखा, जिसकी इतनी समीक्षाएँ छपीं, इतने पुरस्कार मिले और इनसे भी बढ़कर कि उनकी रचनाधर्मिता पर इतने शोध हो गए हैं। कभी-कभी तो यह सब देखकर इतनी हँसी आती है कि मन कह उठता है - ‘कबिरा देखो जग बौराना।’
एक प्रश्न और जो अक्सर वह लोग पूछ बैठते हैं, जो लेखन से नहीं जुड़े हैं और न ही उन्हें लेखन का सौक है। वह कहते हैं –
भाई एक बात बताओ कि यह जो बालसाहित्य की बात हो रही है किसके लिए लिख रहे हैं?
अगर आप कहेंगे कि जाहिर सी बात है बच्चों के लिए लिख रहा हूँ तो वह कहेंगे कि ‘किन बच्चों के लिए? क्या उन तक आपकी रचनाएँ पहुँच भी रही हैं? आप उन्हें इस पर संतुष्ट कर देंगें तो वह आगे कहेंगे कि कितने ‘बच्चों’ ने आपकी रचनाएँ पढ़ीं? प्रश्नों का यह सिलसिला बढ़ता ही जाता है और आप निरुत्तर हो जाते हैं।
वास्तव में आज के तेज गति से बदल रहे बच्चों के लिए बालसाहित्य की रचना करना बड़ा ही दुसाध्य कार्य है। और इससे भी बड़ा जटिल है उन तक अपनी रचनाओं को पहुँचा पाना। इसके लिए हमें सदियों से बने हुए मानकों को बदलना पड़ेगा। यदि आपने यह कार्य कर लिया तो ठीक, नहीं तो बालसाहित्यकार तो आप हैं ही। कुछ तुकबंदी करिए, किसी विद्वान से चाटुकारिता करके उन पर कुछ टिप्पणी करवा लीजिए, छप जाइए और पुरस्कार का जुगाड़ कर लीजिए, लो भाई हो गए बाल साहित्यकार। आज यह चलन बहुत ही आम हो गया है। लेकिन यह बात अपने आप में पूर्ण सत्य नहीं है। हजारों की भीड़ में तमाम सारे ऐसे भी साहित्यकार हैं जो बालमन की सूक्ष्मता से रूबरू हो रहे हैं। उनकी बदलती हुई मनोवृत्ति को पहचान रहे हैं। बदले हुए वातावरण को महसूस कर रहे हैं। बच्चों के सूक्ष्म तर्कों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। उपदेशात्मकता को चित्रण में प्रस्तुत कर रहे हैं। लगातार और बड़ी ही तेज़ी से आधुनिकता की चपेट में आ रहे बच्चों के नवीन नायकों का सृजन कर रहे हैं। साथ ही यदि परम्परा का सृजन कर रहे हैं तो भी उसको संवेदना और मार्मिकता से इतना सहज बना देते हैं कि बच्चा एक बार पढ़कर ही उसको महसूस कर सकता है।
आज के दौर के ऐसे ही दो बालसाहित्यकार भाई हैं - डॉ.मो.अरशद खान एवं डॉ.मो.साजिद खान, जिन्होंने आज के बदलते हुए दौर को बड़ी ही गहराई से महसूस किया और अपने अंतर में उतारा है। इनके बालसाहित्य की बुनावट ऐसी है कि बच्चा तो बच्चा बड़ा भी संवेदना से भर उठेगा। इतना ही नहीं इनकी रचनाओं को वैश्विक आयामों पर भी परखा जा सकता है। आपने अपनी रचनाओं में उन-उन प्रश्नों को उठाया है, जिनसे बड़े-बड़े विद्वान कतराते रहते हैं। आपने उन प्रश्नों को बड़ी ही निडरता के साथ इस प्रकार से चित्रित कर दिया है कि लोग दाँतों तले अंगुली दबा लेते हैं।
यूँ तो इन दोनों खानबंधुओं का संपूर्ण साहित्य ही आधुनिक संवेदना की पूँजी है, लेकिन यहाँ हम केवल उनकी कुछ प्रमुख कविताओं पर ही बात करेंगे। कहानियों आदि पर फिर कभी, क्योंकि सबको एक साथ परखा नहीं जा सकता है।
तो फिर चलिए आरम्भ करते हैं खानबंधुओं की कविताओं की सैर और खोजने का प्रयास करते हैं . . . कुछ मोती।
बड़े-बड़े विद्वान कहते हैं कि बच्चों के साहित्य के लिए रोचकता, सहजता, प्रवाहमयता, गेयता, आकर्षण, मनोरंजकता आदि भाव होने चाहिए। होने ही चाहिए। बिना इनके कोई भी रचना सहज नहीं हो सकती। परन्तु वर्तमान को तो ध्यान में रखना ही होगा। आज का बच्चा कोरी उपदेशात्मकता को गृहण नहीं करता है। वह सीधे-सीधे प्रश्न पूछता है। वह भी इतनी सहजता से कि आप निरुत्तर हो जायें।
डॉ.मो. अरशद खान की एक कविता है ‘रेल के डिब्बे में’। बड़ी ही सहज और मार्मिक, लेकिन जैसे-जैसे आप उसके अंदर उतरते जायेंगे, आप उन-उन प्रश्नों से टकरायेंगे जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। कुछ आगे बढ़ते हुए जब आप पायेंगे कि एक बच्चा ‘राजू’ उन प्रश्नों से जूझ रहा है, जिनसे आज का बुद्धिजीवी भी कतराता-सा दिखता है। तब तो आपकी रही-सही बुद्धि भी जबाव दे जायेगी।
राजू है हैरान रेल के डिब्बे में,
पूरा हिन्दुस्तान रेल के डिब्बे में।
एक सीट पर पण्डित जी हैं
और बग़ल में मुल्ला,
दूजी पर सरदार महाशय
खाते हैं रसगुल्ला।
जैन, बौद्ध, क्रिस्तान रेल के डिब्बे में,
पूरा हिन्दुस्तान रेल के डिब्बे में।
कोई बोले हिन्दी, कोई
उर्दू में बतलाता,
अंग्रेजी-कन्नड़-मलयालम
कोई तमिल सुनाता।
सबका है सम्मान रेल के डिब्बे में,
पूरा हिन्दुस्तान रेल के डिब्बे में।
दो क्षण के इस हेल-मेल में
जुड़ जाते जो नाते,
वही बिछड़ने पर आँखों में
दो आँसू दे जाते।
बना एकता-धाम रेल के डिब्बे में,
पूरा हिन्दुस्तान रेल के डिब्बे में।
डॉ. मो. अरशद खान की बाल कविता ‘रेल के डिब्बे में’ समसामयिक संवेदनाओं से भरी हुई एक ऐसी कविता है, जो बड़ी ही सरलता से आज के लगातार असहिष्णु होते जा रहे वातावरण को आइना दिखा जाती है।
कविता में नायक राजू की हैरानी विविध आयामों पर एक साथ दृष्टिपात करती है। वास्तव में ‘रेल के डिब्बे में’ राजू की हैरानी कोई साधारण सी हैरानी नहीं है, उसकी हैरानी कौतूहल भरी है। उसे लगता है कि जो मुल्ला, पण्डित, सरदार आदि सामाजिक जीवन में पृथक-पृथक दिखायी पड़ते हैं, वह रेल के डिब्बे में इतने अंतरंग क्यों हैं ?
राजू को लगता है कि अरे ! उसके वातावरण में दिखने वाले जो मुल्ला-पण्डित आदि समाज को बाँटने का प्रयास करते दिखते हैं, वह सब यहाँ एक साथ कैसे हैं! उनके बीच की दूरियों को ऐसी कौन सी ताकत है, जिसने मिला दिया है। अपने आप से सवाल करता राजू का कोमल, निश्छल बालमन बड़ी ही सहजता से मनोविज्ञान की गहराइयों में उतर जाता है।
वर्तमान दौर आर्य-अनार्य एवं इस्लामिक संस्कृति के टकराव और उत्सर्जन का दौर है। तमाम सारी परम्परायें बिखर रही हैं। वर्ग तथा समुदाय टूट रहे हैं। आदर्श खण्डित हो रहे हैं। निगाहें ‘शक’ उगल रही हैं; ऐसे में राजू देखता है कि उसके समय के दो प्रबल प्रतिद्वन्दी(पण्डित और मुल्ला) एक सीट पर प्रेम से बैठे हैं। सरदार जी द्वारा ‘रसगुल्ला’ खाना उनकी आपसी मिठास को शक्ति प्रदान करता है, जिसमें अन्य सभी अर्थात् बौद्ध, जैन, क्रिस्तान आदि भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।
राजू की दृष्टि और भी गहरे में उतरती है। उसे लगता है कि ‘अरे यह क्या!’ रेल के इस डिब्बे में तो भाषा-बोली को लेकर भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जबकि समाज में यह सब अलग-अलग दिखती हैं। कोई हिन्दी के लिए लड़ा-मरा जा रहा है तो कोई किसी अन्य बोली-बानी की वकालत कर रहा है।
वास्तव में राजू महज परियों के पंखों पर उड़ने वाला पुरातन बच्चा नहीं है। वह तेज़ी से बदल रहे वैज्ञानिक युग का लड़का है, जिसकी नजर तर्क सागर की गहराई में उतरना चाहती है। वह तब तक तर्क करना चाहता है जब तक उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हो जाती है।
इतना सब कुछ देखने-समझने के बावजूद राजू परेशान हो उठता है। अब तक की उसकी हैरानी, मार्मिक परेशानी में बदल जाती है। उसे अपनी दृष्टि और समझ पर अनायास ही भ्रम होने लगता है। कल्पना और तर्कों में उड़ता-तैरता उसका मनोमस्तिष्क अचानक ज़मीन पर आ गिरता है। उसे लगने लगता है कि यह सब बकवास है, दिखावा है, छल है। वास्तविकता यह है कि यह सब एकमेव नहीं हो सकता है क्योंकि एकमेकता परिस्थितिगत है। यह अंदेशा अनायास ही उसकी आँखों को नम कर जाता है।
बावजूद इसके संपूर्णता में देखें तो डॉ. खान कविता में अपना सकारात्मक आशावादी संदेश सहजता के साथ दे जाते हैं। यथार्थ एवं कल्पना के बीच आशा का संचार करती यह कविता बाल साहित्य की बेजोड़ रचना है।
कुछ इसी प्रकार के भाव से बंधी लेकिन एक पृथक वातावरण को इंगित करती कविता डॉ. मो. साजिद खान की ‘खुशियाँ लाई ईद’ है, जो वर्तमान वातावरण पर बड़े ही सहज व्यंग्य से एक करारा थप्पड़ जड़ जाती है। थप्पड़ भी ऐसा जिसे खाकर बड़े से बड़ा बुद्धिजीवी दाँत दिखाता रह जायेगा। समाज को तोड़ने वाले समस्त साधन ध्वस्त हो जाते हैं।
फिर तो सोनू, मोनू, पंकज
मिलने आए ईद
पहले अब्दुल गले मिला फिर
मिलने लगा फरीद।
सबने खूब सिवइयाँ खाईं
जमकर मज़ा उड़ाया,
खुशियाँ संग में लेकर अपने
यह त्योहार है आया।
आज समाज को तोड़ने वाले यमराज अपनी लाल-लाल आँखें फैलाये हुए हर दिशा में अपना साम्राज्य फैलाए हुए आसनाशीन हैं। ऐसे विशाक्त वातावरण में सोनू, मोनू, पंकज का अपने अज़ीज़ अब्दुल और फरीद के घर ईद मिलने जाना, उनसे गले लगना और ‘बेझिझक’ सेवइयाँ खाना वास्तव में बड़े हिम्मत का काम है।
कविता में कोरी उपदेशात्मकता आधुनिक होते जा रहे बच्चों को उबाती है, इसलिए उसमें भावों का चित्रण होना उसको मजबूत बनाता है। खानबंधुओं की कविताओं में इसका बड़ा खयाल रखा गया है। इनकी लगभग समस्त कविताओं में भावों के चित्रण की प्रधानता है।
डॉ.मो.अरशद खान की एक कविता है ‘ऐसा पेड़’, जिसमें बड़ी ही सहजता से उन्होंने आधुनिक समस्याओं को इतने कायदे से पिरो दिया है कि कविता बच्चों के लिए तो मनोरंजन प्रधान हो गई है, वहीं आधुनिक समाज और उसके बुनकरों के लिए तमाम प्रश्न छोड़ जाती है।
एक डाल पर फले संतरा
और एक पर आम,
एक डाल पर लाल मुनक़्क़ा
दूजी पर बादाम।
एक पेड़ में सारी चीज़ें
काश कभी लग पाएँ!
कहाँ बची अब जगह पास जो
इतने पेड़ लगाएँ ?
डॉ.मो. अरशद खान अपनी कविताओं में बड़ी ही सहजता से मानवीय संवेदनाओं को पिरो देते हैं। उक्त कविता में आपने जहाँ एक ओर तमाम विभिन्नताओं को एक प्लेटफार्म देने की बात कहकर भारत में बढ़ती असहिष्णुता पर अपना मार्मिक छोभ प्रकट करते हुए एकता की बात करते हैं तो दूसरी ओर चलते-चलते लगातार सिमटती जा रही ज़मीन और लगातार कट रहे वनों पर भी अपनी चिंता जता दी है। उक्त कविता कहने को तो बालकविता की श्रेणी में आती है, लेकिन भाव इतने गंभीर कि तमाम समसामयिक समस्याओं को बड़ी सहजता से आइना दिखा जाती है। आपने सिद्ध कर दिया कि ‘केवल मनोरंजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए।’
आज जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव के चलते जल, जंगल और ज़मीन सब के सब सिकुड़ते जा रहे हैं। आज ईंटों के दिखावटी जंगल गढ़े जा रहे हैं। प्रकृति का विराट स्वरूप हमसे पृथक होता जा रहा है। नानी के गाँव का विशाल बरगद, जो बच्चों की छुट्टियों का गवाह और खेल का साथी था, निगाहों से ओझल हो गया है। तरह-तरह के करतब दिखाने वाले बन्दर मामा की उछल-कूद के लिए पेड़ ही कम होते जा रहे हैं। बच्चों की छुट्टियों को मादकता से भरने वाले आम, जामुन, शहतूत आदि के पेड़ कट चुके हैं। हरा-भरा सा वातावरण धूल उड़ाता-सा प्रतीत होने लगा है। बच्चों के बचपन की सहचरी प्रकृति आज ऐसा लगता है जैसे कि छोटे-छोटे घरों के गमले में समाती जा रही हो। डॉ.मो.साजिद खान की कविता ‘क्या गमले में उग सकता है आम?’ कई प्रश्न हमारे सामने छोड़ जाती है।
मम्मी! क्या मेरे गमले में
उग सकता है आम?
जिस पर बंदर मामा करते
दिन भर खेल तमाम?
बच्चा अपनी माँ से बड़े ही मासूम से सवाल करता है –
जो नानी के गाँव लगा था
बरगद प्यारा – प्यारा,
और द्वार पर नीम, ताप में
देता बड़ा सहारा!
दाढ़ी वाले बरगद बाबा
पीपल मंदिर वाला,
वह इमली का बड़ा पेड़, वह
महुआ टीले वाला!
वैसा ही क्या लॉन हमारा
बन सकता है धाम?
तोतों की टें-टें, कोयल की
मीठी-मीठी बोली,
वे बगुलों की बड़ी कतारें
मोरों की वह टोली!
हरे-भरे वन बाग़ लहकते
जामुन बहुत दुलारा,
वही चाहिए, वही चाहिए
माँ! सब प्यारा प्यारा!
नहीं चाहिए लिली, कैक्टस
और उगा यह पास!
बदलते हुए वातावरण ने सबकुछ बदल दिया है। दिखावे की संस्कृति ने हमारे मनोमस्तिष्क पर इस कदर अपनी जड़ें जमा ली हैं कि हम उससे आगे बढ़कर कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। बच्चे के सामने से दादी-नानी की कहानियाँ दूर हो गई हैं और उनके साथ ही दूर हो गया है वह सब भी जो उनके सानिध्य में बच्चा महसूस करता था। गाँव का वह बरगद, जिसके तले गुड्डे-गुड़ियों का खेल होता था, संवेदना का वह मिलन जो बच्चों को ताउम्र बाँधे रखता था। जिस स्थान पर आस-पड़ोस के तमाम बच्चे एकत्र होते थे, अब नहीं रहा। हमारी संवेदनाओं के प्रतीक द्वारे का नीम, मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ दाढ़ी वाले बरगद बाबा, मंदिर वाले पीपल देवता, इमली का बड़ा पेड़, टीले वाला महुआ सब कुछ आज की मर रही मार्मिकता की भेंट चढ़ गया है।
बच्चा इन संवेदनाओं के तारों को अपने लॉन में बैठा हुआ अपनी कल्पनारूपी धागे में पिरो रहा है। वह सोचता है कि काश! कि यह सब उसके गमले में समा पाते। काश! कि यह सब उसके आस-पास झूम उठते।
कविता में आए कैक्टस और लिली आदि बाजारवादी सोच के वह प्रतीक हैं जो हमारे दिमाग में गहराई से उतरते जा रहे हैं। यह वह हथियार हैं, जिन्होंने तोतों का गला घोट दिया है। कोयलों के गले की नाल को उखाड़ फेंका है। सहज प्रकृति को उजाड़ दिया है।
कुछ इन्हीं भावों से भरी हुई डॉ.मो.अरशद खान की एक कविता है – ‘सूना सूना सा लगता है अब नानी का गांव’।
आज भूमण्डलीकरण के दौर में गांव अपनी मूल संवेदना से अनायास ही कटते जा रहे हैं। गावों की प्रकृति के साथ ही वहाँ का मेल-मिलाप भी अब बदला-बदला लगने लगा है। वर्तमान की विषाक्त राजनीतिपूर्ण वातावरण ने गाँवों तक से उनकी उस संवेदना को उखाड़ फेंका है, जिससे गाँव के सब छोटे-बड़े एक डोर में बंधे रहते थे।
बाल साहित्यकार ने ग्रामीण संवेदना को बड़ी गहराई तक महसूस किया है। पिछले दस सालों से जब आज के गांव को देखता हूं तो बस यही दिखता है........
दूर-दूर तक हरा-भरा जो
फैला था मैदान।
लालाजी ने बनवा ली हैं,
वहां कई दूकान।
बनकर ठूंठ खड़ा है पीपल,
जो देता था छांव।
माली बाबा की फुलबारी
सूख गई अब हाय!
रामदीन का लड़का अब तो
वहां चराता गाय।
सूख गई वह नदिया प्यारी,
जिसमे चलती नाव।
हमें सुनाता था जो जंगल
पुरवइया में गान,
चुभता है अब आंखों में वह,
बनकर रेगिस्तान।
कोयल की अब कुहुक नहीं बस,
सुन पड़ती है कांव।
गाँव का चुनाव हो गया, जिसमें पूरा गाँव कई दलों में विभाजित हो गया। जो रामचरन अभी तक मंदिर पर मनाये जाने वाले शिवरात्रि आदि उत्सवों में दिल खोलकर नाचता-गाता था, अब उसके लिए वह मंदिर सवर्ण का मंदिर हो गया है। जो पुरोहित बाबा गाँव के हर घर में सत्त्यनारायण की कथा सुनाया करते थे, उनके लिए गाँव के तमाम घरों से ‘दलित सी’ बदबू आने लगी है। वलीउल्ला मनिहार, छुटन्ने खाँ दूधिया और बगिया वाले रहीम चच्चा सफेद कुरता-धोती की अपनी पोशाक में दोनों समुदायों को एक धागे में बाँधे रहते थे, आज गोल टोपी लगाने पर मज़बूर हो गए हैं। चुनाव के बाद ताकत आ जाने पर लाला जी ने गाँव में बच्चों के खेलने के स्थान खड़े बरगद को कटवाकर कई दूकाने बनवा ली हैं। हरा-भरा मैदान गया सो गया ही, दुआरे पर खड़ा पीपल का पेड़, जिसके तले शिव जी के सानिध्य में रानी, मीरा, खलोली, अकरम और फरीद के साथ जो खेल खेल जाते थे, सब समाप्त हो गए हैं। रानी और मीरा का ब्याह हो गया है। खलोली और फरीद बाहर चले गए हैं और अकरम दूसरी पार्टी से संबंधित है। पीपल बाबा ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उनके नीचे का यह सौंदर्य कभी समाप्त भी होगा, लेकिन क्या करें! बदली हुई हवा ने सब कुछ समाप्त कर दिया। जड़ के घेरे में बैठे शिव जी कहीं और चले गए, सिर की शोभा बगुलों का भी वहाँ मन नहीं लगा। अब पीपल बाबा क्या करें। आत्मरस निचुड़ गया। सूख तो जायेगे ही।
माली दादा की फुलवारी मुरझा गई, रामदीन का चारागाह सूख गया और तो और सदा नाव को अपने जल प्रवाह से हिचकोले देने वाली नदी भी सूख गई। पुरवइया की तानों पर संगीत छेड़ने वाला जंगल आधुनिक बाज़ार की बलि चढ़ गया। वहाँ एक बड़ी फैक्टरी लग गई और जो स्थान हमेशा महकता रहता था, वहाँ आज धूप की प्रेतात्माओं का परिभ्रमण आरम्भ हो गया है। कोयल की मीठी कूक अब ‘कड़वी काँव’ में बदल गई है।
आश्चर्य होता है कि एक बालकविता कही जाने वाली रचना अपने हृदय में इतनी गहन संवेदनाओं को समाये हुए हैं। क्या किसी ने कवि के मासूम से हृदय को टटोलने का प्रयास किया है? पल-पल मरने के बाद कहीं संवेदनाओं को शब्दों का जामा पहना पाया होगा। अद्भुत !
डॉ.मो. अरशद खान का एक पात्र अपने बचपन के गाँव से दूर . . . बहुत दूर अपने छोटे से ‘रीडिंग रूम’ में बैठा हुआ गाँव के अपने मित्र को एक खत लिख रहा है। अपने व्यस्त से समय में से तनहाई का कुछ समय निकालकर शहरी मित्र क्या-क्या याद करता है . . . ‘गिरधर भैया अपने हाथों पाती मुझको लिखना।’
लिखना अबकी बार खेत में, कैसे आए धान,
देर रात तक दादा गाते, अब भी लम्बी तान?
गऊघाट के मेले से तुम, क्या-क्या लेकर आए,
काली गैया के बछड़े क्या बड़े-बड़े हो आए?
सांझ ढले तक खेल-खेलते, अब भी सुखना-दुखना?
चौपालों में देर रात तक, होते हँसी-ठहाके?
क्या रामू काका मानस की, चौपाई हैं गाते?
बूढ़े दादा से तुम सबने, कितनी सुनी कहानी,
लिखना उनसे बात ज्ञान की, तुमने कितनी जानी।
सीख लिया अब कल्लू ने क्या, अ-आ-इ-ई पढ़ना?
जल्दी करना देर न करना, पाती झट भिजवाना,
टूटी-फूटी भाषा में ही, सबका हाल बताना,
फिर मत पूछो पाती पाकर, मन कितना खुश होगा।
नहीं दिया पाती, सोचो, दुख मुझको कितना होगा,
हरकारे की राह ताकती रहती तेरी बहना।
कितना गहरा दर्द है, जिसको केवल कवि ही समझ सकता है। अपने वस्तु-विन्यास में इसको कोई बाल कविता कहे तो कहे मैं ना कहूँगा ‘बालकविता’। हमें तो अपने वजूद से कटा एक वयस्क कवि रोता, सिसकता दिखाई दे रहा है। और इस तरह से कि उसके रोने-सिसकने का कोई मतलब भी नहीं है। कौन देखता है कि एक बालकवि इस तरह से सिसक रहा है। उसे एक-एक कर वह समय याद आ रहा है जिसने उसे गढ़ा है। उसे वह सब कुछ याद आ रहा है जो उसके हृदय में आज भी कसक बनकर समाया हुआ है। मुझे लगता है कि कवि अपने आधुनिक ‘ड्रॉइंग रूम’ में रोया होगा दहाड़ें मार-मारकर। उसका रक्त उबला होगा सब कुछ देखकर। तन गई होंगी उसके मस्तिष्क की नसें मुक्तिबोध के माफिक। अब जब मार्मिकता इतनी गहन है तो आधुनिक से आधुनिक बच्चा भी उससे बिंधे बिना न रह पाएगा उसके समक्ष भी वह तमाम बिंब सजीव हो उठेंगे, जो कवि ने महसूस किए हैं।
अब समीक्षा . . . हमारे जीवन में पत्रों का बड़ा स्थान है। पत्रों की संवेदना को आज के मोबाइल युग के संसाधनों से नहीं महसूस किया जा सकता। प्रसिद्ध बाल साहित्यकार डॉ.मो.अरशद खान अपनी कविताओं में ग्रामीण संवेदना को कुछ इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि पूरा अंचल ही सजीव हो उठता है और साथ ही आंखों की कोरों को गीला भी कर जाता है।
कविता कई बिंब हमारे सामने प्रस्तुत करती है, जो हमारी आँखों के सामने ज्यों के त्यों सजीव हो उठते हैं। बच्चा जानना चाहता है कि इस बार खेतों में धान कैसे हुए? उसके हृदय में चिंता है कि कहीं, टी.वी. पर दिखाया जा रहा है कि इस बार अधिक वर्षा के चलते धान की जो फसलें समाप्त हो गई हैं, उसके गाँव का हाल भी तो वही नहीं हैं? आशंका से उसका कोमल हृदय काँप उठता है। आधुनिक बच्चा टी.वी. पर रोज ही देखता-सुनता है कि फसल बर्बाद होने से इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, इतने किसानों का सर्वस्व उजड़ गया!
वह आगे बढ़ते हुए जिज्ञासा प्रकट करते हुए जानना चाहता है कि क्या अब भी देर रात तक ‘पोर’ पर ठहाके गूँजते हैं? क्या अब तक दादा देर रात तक गाना सुनाते हैं? ‘पहने कुरता पर पतलून आधा सावन आधा जून’ याद करके उसकी आखें डबडबा आती हैं।
जिज्ञासा उठती है कि क्या अब भी सुबह-सकारे गाँव में सबसे पहले उठकर रामू काका मानस की चौपाइयाँ गा-गाकर सुनाते हैं – ‘भये प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशिल्लिया हितकारी, हरषित महतारी, मुनि मन हारी, अद्भुत रूप बिचारी....’ दूर कहीं दिशा-पाखाना जाते हुए किसी से ‘जय राम जी की’ कहने के बाद रामू काका वापस चौपाइयों पर आ जाते हैं – ‘श्री रामचन्द्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम. . . ’ बाल कविता की यह संवेदना! कवि पल-पल रोया होगा।
इन सब भावनाओं से अपने आपको कुछ बाहर निकालता हुआ कवि मन लिखने लगता है कि क्या कल्लू ने अ-आ-इ-ई पढ़ना सीखा है?, क्या आज भी गऊ घाट पर मेला लगता है?, क्या आज भी गाँव के बच्चे साँझ ढ़ले एक साथ उधम मचाते हैं?, क्या काली गइया और उसका बछड़ा आज भी गला सहलाने पर वैसे ही झूम उठता है? और सबसे बढ़कर कि क्या आज भी गाँव के बूढ़े दादा सब बच्चों को एक साथ बिठाकर कहानियाँ सुनाते हैं? न जाने कितने प्रश्न और जिज्ञासायें भरी पड़ी हैं बालमन में।
कवि को पता है कि अब यह कुछ नहीं बचा है। सब कुछ बदल चुका है। पर मन का क्या करे जो अब तक उस संवेदना से बंधा हुआ है। अंत में थक-हारकर कवि अपने मन से यह कहते हुए कि, ‘हमारी पाती का उत्तर जल्द ही देना मैं प्रतीक्षा करूँगा’, पाती को रख देता है। आगे चलकर देखता है कि अरे यह क्या? यह तो कविता बुन गई! कुछ आश्चर्य, कुछ अफसोस! बहरहाल कर भी क्या सकता है। अपने बच्चों में अपना बचपन देखकर ही संतोष कर लेता है।
आज हम उस दौर से गुजरते जा रहे हैं जहाँ परिवार सूक्ष्म से सूक्ष्म होते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार एकल में परिवर्तित होते जा रहे हैं। संयुक्त परिवारों के बच्चों के जहाँ ऊपर दादा-दादी, नाना-नानी, ताया-ताई और चाचा-चाची का ममत्त्व झलकता रहता था वहीं एकल परिवारों के बच्चे अपने सगे माँ-बाप के कुछ पल के सानिध्य तक के लिए तरसते हैं। दादा-दादी और नाना-नानी अब बच्चों के अपने परिवार से अलग हो गए हैं। उनका अब एक अलग घर और गाँव हो गया है। इससे बच्चे उनकी सीखों और कहानियों से भी अलग हो गए हैं। ऐसे वातावरण में बच्चों के अंदर से संवेदनशीलता का समाप्त हो जाता कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
पहले संयुक्त परिवार में ‘कजिन’ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। सब आपस में छोटे-भाई बहन हुआ करते थे। चाहें चाचा के हों या ताऊ के। चाचा-ताऊ भी कम ही होते थे, होते थे छोटे पापा और बड़े पापा, छोटी मम्मी और बड़ी मम्मी। आधुनिकता ने सबको डस लिया है।
डॉ.मो. अरशद खान की ही एक कविता (रक्षाबन्धन) और है जो भाई-बहन के आपसी प्रेम को कितनी सूक्ष्मता से व्यक्त करती है।
भइया रक्षाबन्धन पर तुम
क्या दोगे उपहार
चंदा दोगे – तारे दोगे
या दोगे संसार।
वह धागा जिसे कोई तोड़ नहीं सकता है। बहन के द्वारा माँगे गए उपहार भाई कैसे मना कर सकता है –
सुन लो भैया नहीं चाहिए
खेल-खिलौने ढेर,
मेरे ऊपर कर देना तुम
बस इतना उपकार।
विनती मेरी इतनी-सी बस
जाना चाहे दूर,
नहीं भुलाना इस बहना को
करते रहना प्यार।
आज स्नेह का यह धागा कमजोर-सा पड़ता प्रतीत हो रहा है। कविता किशोर मन की वास्तविक अभिव्यक्ति है। कविता में संयुक्त परिवार के टूटने की कसक साफ सुनाई पड़ती है।
बच्चों के बचपन का गवाह पीपल का पेड़ और उसके घेरे में गुड्डे-गुड़िये का मनमोहक खेल। क्या मनोहारी बिंब होता था बचपन का, जहाँ सारी दूरियाँ बौनी पड़ जाती थीं। डॉ. मो. अरशद खान की कविता में गुड़े-गुड़िया के खेल का जितना मोहक चित्रण दिखता है, उससे कहीं अधिक उसके निहतार्थ भी दिखाई देते हैं।
डेढ हाथ का काढ़े घूँघट,
सोने के गहनों से सज-धजकर,
बैठ पालकी गुड़िया रानी,
आज चली ससुराल।
सुंदर है माथे का टीका,
नथ के आगे चंदा फीका,
चमके चम चम चुनरी प्यारी,
और गरारा लाल।
इस संवेदना को तो वही समझ सकता है, जिसने बहन या बेटी को विदा किया हो। एक-एक शब्द गहन संवेदना से बिंधा हुआ।
सहज शब्दों में गहन भावों को व्यक्त कर देना एक सच्चे रचनाकार की सच्ची सफलता है। ऊपर-ऊपर छोटी-सी और महज मनोरंजन प्रधान सी दिखने वाली डॉ. मो. साजिद खान की कविता ‘ अप – टू – डेट चूहेराजा' वास्तविक अर्थों में अपने कलेवर में वैश्विक संवेदनाओं और उससे उलझी समस्याओं को समेटे हुए है।
चूहे राजा घर से निकले
जाने को रंगून,
कोट पहनकर टाई बाँधी
पहन लिया पतलून।
‘शू’ भी प्यारा-प्यारा पहना
और लगाया ‘हैट’
ख़ूब तैयारी करके बोले –
मैं हूँ – ‘अपटूडेट।’
लगे झूमने तब शीशे में
अपनी सूरत देख,
सोचा, इस दुनिया में सुंदर
मैं ही हूँ बस एक।
अब तो सारे जंगल भर में
मेरा होगा राज,
तभी अचानक आते देखा
बड़ा भयानक बाज़।
भूल हेकड़ी भागे, ठोकर –
खाकर गिरे धड़ाम,
चूहे राजा का बिगड़ा था
फिर तो सारा काम।
भूल हुई, दादी का चश्मा
पहन चले थे आज,
इसीलिए तो नन्हीं चिड़िया
उन्हें दिखी थी बाज़।
‘अप टू डेट चूहेराजा’ देखने-पढ़ने में तो एक बाल कविता लगती है और है भी, क्योंकि बाल साहित्य की सबसे मूल शर्तें – सुलभता, मनोरंजकता और मार्मिकता यह कविता बडी ही सहजता से पूरी करती है, पर कविता यहीं नहीं रुकती है, वह और भी काफी आगे तक जाती है। चूहा, रंगून, कोट, टाई, पतलून, शू, हैट, जंगल, राज, बाज, नानी का चश्मा, नन्हीं चिडिया आदि सहज से दिखने वाले शब्द अपने आप में वर्तमान की तमाम समस्याओं को अपने प्रतीकार्थ में समेटे हुए हैं। वर्तमान राजनीति से लेकर मीडिया तक, जहाँ छोटी से छोटी बात को चिडिया के स्थान पर बाज बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है, को डॉ. मो. साजिद खान बड़ी सहजता भरे व्यंग्य के माध्यम से मसखराना अंदाज़ में प्रस्तुत कर देते हैं। जब जनता को चिडिया और बाज का भ्रम समझ में आ जायेगा तो चश्मों की सारी हेकडी खुद व खुद निकल जायेगी।
वास्तव में आज का बच्चा वो बच्चा नहीं रहा जो कोरे उपदेशों को स्वीकार करेगा। वह आपकी बात को अपने तर्कों पर तौलेगा, जायजा लेगा, तब कहीं जाकर उसे अपनी स्वीकृति देगा। आज के तेज़ी से जवान हो रहे बच्चों के लिए बालसाहित्य में कोरी उपदेशात्मकता के स्थान पर भावों की गंभीरता और सहज संवेदना को अधिक स्थान मिलना चाहिये।
कुछ इसी भाव बोध और खासकर वर्तमान मीडिया की करतूतों को उजागर करती डॉ. मो. अरशद खान की एक कविता है – ‘पढ़ा आज अखबार में’। कविता कलेवर में बालकविता भले ही हो, पर बालसुलभता से हँसा-हँसाकर वैश्विक स्तर पर मीडिया की पोल खोल देती है।
पढ़ा आज अख़बार में ?
ट्रक सीधे बस से टकराया
बारह घायल चार मरे,
बैंक-डकैती, लुटे करोड़ों
सब हैं सहमें डरे-डरे।
दो घायल तकरार में।
पढ़ा आज अख़बार में ?
आज यहाँ निकलेगी रैली
आज वहाँ होगी हड़ताल,
बन्द रहेगा शहर, दुकानों
में देंगे सब ताले डाल।
दस लोगों को पुलिस ले गई
सीधे कारागार में।
पढ़ा आज अख़बार में ?
कल फिर कर्फ़्यू लगा शहर में
सड़कों पर सन्नाटा है,
भाई-भाई को कुछ लोगों
ने देखो फिर बाँटा है।
बही ख़ून की नदियाँ देखो
होली के त्यौहार में
पढ़ा आज अख़बार में ?
कभी-कभी सोचता हूँ कि भविष्य में जब आधुनिकता का इतिहास लिखा जायेगा तो उसका सबसे बड़ा गवाह मीडिया होगा। अखबार बयाँ करेगा कि किसने, कब, कौन-सा बड़ा कार्य किया अथवा नहीं किया। लेकिन सब जानते हैं कि अखबार का सच कितना सच है!
अखबार ‘बारह घायल, चार मरे’ ऐसे कह देता है जैसे कि मरने वालों के अंदर कोई संवेदना ही न हो? अखबार की यह संवेदन-शून्यता ही भविष्य की संवेदना का विकास करती है। आज अभिव्यक्ति की अजादी का दम भरा जा रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। वास्तविक अर्थों में आज ‘सब हैं सहमें डरे-डरे।’ इस डर के पीछे यह मीडिया कुछ कम जिम्मेवार नहीं है। संज्ञा-शून्यता का इससे वीभत्स्य दौर क्या हो सकता है कि दुकानों के साथ-साथ हृदयों में भी ताले पड़े हुए हैं। एक भाई दूसरे भाई पर जान निछावर कर रहा है, इसके बजाय इस पर अधिक जोर दिया जा रहा है कि ‘भाई-भाई को कुछ लोगों ने देखो फिर बाँटा है।’ और जोर देकर दिखाया जाता है कि देखो गजब हो गया ‘बही ख़ून की नदियाँ देखो होली के त्यौहार में’।
कहने को बाल कविता है, पर है बन्दूक की गोली। जा लगेगी सीधे निशाने पर।
आज के बच्चों के सामने एक सबसे बड़े समस्या यह है कि आज की शिक्षा-व्यवस्था ने उनका बचपन छीन लिया है। आज के बच्चे माँ-बाप के लिए किसी विजनिस से कम नहीं हैं। माँ-बाप उनको शिक्षा नहीं देना चाहते हैं बल्कि प्रतिस्पर्धा के चलते उन्हें अपनी ‘नाक’ का प्रतीक बना लेते हैं। उन्हें लगाता है वह बच्चे पर जितना ‘इन्वेस्ट’ करेंगे, बच्चा उन्हें उतना ही ‘आउटपुट’ देगा। इसके चलते वह यह नहीं सोचते कि बच्चे की सुकुमार संवेदना पिस रही है। वह प्रेशर कुकर बनता चला जा रहा है। माँ-बाप उसे अपने तरह से ढालना चाहते हैं। बच्चे के मन को समझने का प्रयास कभी नहीं करते हैं। उन्हें तो बच्चे में केवल एक ही वस्तु दिखती है और वह है प्रतिस्पर्धा। डॉ.मो.साजिद खान की कविता ‘क्या अच्छा लगता है’ का नायक बच्चा बड़ी हिम्मत के साथ अपने आधुनिक अभिवावक के समक्ष मुँह खोलने का प्रयास करता है। उसके हृदय का विद्रोह कुछ इस प्रकार से फूट पड़ता है।
दीदी कहती है कम बोलो,
चलो, फटाफट पुस्तक खोलो।
नहीं खेलना, हरदम पढ़ना
क्या अच्छा लगता है ?
मम्मी-पापा का है कहना,
मेरा सपना पूरा करना।
अपने जैसा सबको गढ़ना
क्या अच्छा लगता है ?
दद्दा मुझको पीटा करते,
पापा उनको कुछ न कहते।
गुस्से में दद्दा से लड़ना
क्या अच्छा लगता है ?
मम्मी-पापा जब भी लड़ते,
दो चाँटे मुझको भी पड़ते।
सोचो, ऐसे में कुछ पढ़ना
क्या अच्छा लगता है ?
एकल परिवारों के पति-पत्नी का आपसी व्यवहार मासूम मन पर किस कदर विद्रोह की रेखायें खींच देती हैं, कविता के अंतिम बन्ध से बखूबी समझा जा सकता है।
आज का अध्यापक भी अपनी जिम्मेदारियों से भटक गया है। वह नन्हें-नन्हें बच्चों के मनोभावों को समझने वाला अध्यापक कम, विद्यालय में नौकरी करने वाला ‘नौकर’ अधिक होता जा रहा है। बच्चा किताबों और उनको रटने का ‘प्रेशर’ डालने वाले अध्यापक के सामने बेबस-सा नजर आता है। डॉ.मो.अरशद खान की कविता ‘कुछ तो दया करो’ इस बेचारगी से बच्चे के मनोभाव को व्यक्त करती है कि व्यक्ति सोचने को मजबूर हो जाए कि वास्तव में आज के बच्चे का बचपन आज की शिक्षा-प्रणाली के तले कुचलता जा रहा है।
सात किताबें – आठ किताबें
और किताबें दस,
पढ़ते लिखते, लिखते पढ़ते
ऊब गया मैं बस !
होमवर्क ही करते – करते
दिन तो बीत गया,
भोले बच्चों पर मैडम जी
कुछ तो करो दया !
वास्तव में देखा जाए तो असल बात यह कि बाल साहित्य लिखना ही बड़े बूते की बात है और उस पर भी अधिक बूते की बात है उसमें उन मानवीय संवेदनाओं को समेट पाना, जो सार्व भौमिक हों। वह व्यक्तिगत न होकर समष्टिगत हो जाए। उसके आयाम क्षेत्रगामी से विश्वव्यापी हो जाएं। कलेवर कैसा भी हो लेकिन उसका भाव गहन ही हो। साथ ही वह गहन भाव कोरी उपदेशात्मकता से लबरेज न होकर चित्रणप्रधान हो। मार्मिकता उसकी पूँजी हो और मनोरंजन उसके कलेवर का अहम हिस्सा हो। यह तमाम चीजें खानबन्धु डॉ.मो.साजिद खान एवं डॉ.मो.अरशद खान की कविताओं की प्राण हैं। यही वह शक्ति है, जो आपकी बाल सी लगने वाली कविताओं में वैश्विक आयाम भर देती है।
मानस स्थली
सीनियर सेकेण्डरी रेजीडेंसियल पब्लिक स्कूल
फरीदपुर, बरेली (उ.प्र.)
manavsuneel@gmail.com
For Call : +91 9307015177
For WhatsApp : +91 9918992511
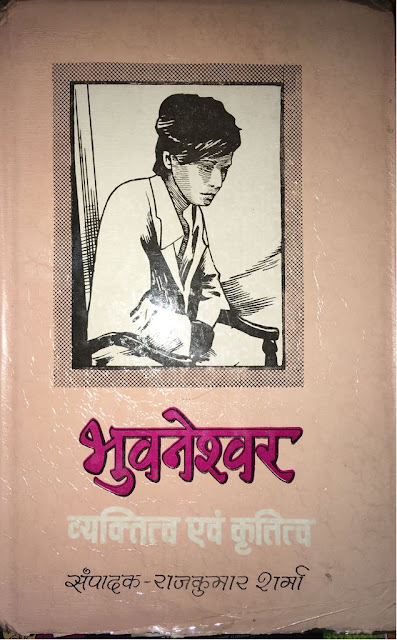
Comments
Post a Comment