वाम का चरित्र बनाम चरित्र का वाम
यह आलेख मेरे बाबा का है जो कथा प्रतिमान पत्रिका में छद्म नाम से छपा था..............
वाम का चरित्र बनाम चरित्र का वाम
आचार्य भिक्खुमोग्गलायन
शीतल प्रसाद इस छोटी सी बात को मोटी तौर पर मान कर चलता है कि लेखन और प्रतिबद्ध, ये दोनों ही शब्द हिन्दी के लेखक और पाठक(!) के परिचित शब्द हैं। यह बात दूसरी है कि लेखक अपने ‘लेखक’ की गरिमा को बनाए रखने के लिए पाठक से एक समानान्तर दूरी बनाए रखता है। उसे उसकी समझ पर भी बराबर सन्देह बना रहता है और समानान्तर रेखाओं के बाल सुलभ उदाहरण ‘रेल की पटरी’ की तरह लेखक और पाठक सुदूर लक्ष्य तक कभी और कभी नहीं मिल पाते। अपनी समझ पर कुछ गंभीर टाइप का विश्वास करके वह कभी-कभी तो ऐसी सूक्तियां उछाल देता है कि पाठक दोनों हाथ ऊपर उठाये आकाश को ताकता रह जाता है और सूक्ति है कि शून्य में झूलती रहती है। उदाहरण के लिए एक वाम पक्षधर लेखक ने एक सूक्ति उछाली-अच्छी कहानी वाम होने के लिए बाध्य है।
अब बात साफ है कि लेखक ने कहानी का चरित्र, एक कैरेक्टर तय कर दिया-वाम। वाम है तो वह एक अच्छी कहानी है अन्यथा बस कहानी है। यानी गुणात्मकता की दृष्टि से वाम मुख्य है और कहानी गौण। और जब वह गौण ही है तो वह चाहे न भी हो तो भी चलेगा। परिणाम यह हुआ कि इस सूक्ति कथन में विश्वास करने वाले लेखक की अनेक कहानियों में से कहानी गायब। कहानी गायब का अर्थ वहाँ से वह बुनावट (शिल्प) गायब जो उसे विश्वसनीयता प्रदान करे। केवल वाम मौजूद। अब जरा पाठक की नियति देखिए। वह कहानी पढ़ने के लिए कहानी को पढ़ना आरंभ करे और उसे ढूढंता हुआ कहानी के अंत तक पहुंचे। अपना समय और धन, दोनों को वह खर्च करे कहानी के लिए और अंत में पाए क कहानी ही नदारद तो उसकी खीझ आखिर किस पर उतरे। वह ‘वाम’ को पढ़ने के लिए तो अपना समय और धन खर्च करने नहीं बैठा है। और अगर कभी ‘वाम’ ही पढ़ने को उसका मन करेगा तो क्या वाम की बाजार में कमी है। ‘पार्टी मेनीफेस्टो’ से लेकर ‘मार्क्सवादी सौन्दर्यशास्त्र’ तक एक से एक धाँसू पुस्तकों के डीलक्स संस्करण से बाजार पटा पड़ा है। वह कहीं से कुछ उठा लेगा। वैसे कम मजेदार तथ्य यह भी नहीं है कि अपना माल निकालने के लिए पूंजीवादी ‘सेल’ हथकंडे का प्रयोग करते हुए वाम के विक्रेता अपने इस ‘वाम’ के माल को काफी सस्ता और आकर्षक गेट-अप में बेंचते हैं। अब जबकि शुद्ध माल बाजार में काफी सस्ता उपलब्ध रहता है, इस माल को बैसाखी बनाकर चलने वाला लेखक की कहानी-उपन्यास वाला माल काफी महँगा पड़ता है। सम्पन्नता बटोर कर लेखक से प्रकाशक बने ये वाम साहित्यकार देश की गरीब जनता की क्रय शक्ति का भी आंकलन नहीं कर पाते। अपने प्रकाशन के मैनेंजिंग डायरेक्टर बने और अपने पूरे उपक्रम में स्वयम् अपने लिए मोटा वेतन तय करने वाले ये साहित्यकार अक्षर-अक्षर जिस साहबी जिंदगी को जीते हैं वह सचमुच दिव्य है। अलौकिक है। इनकी पुस्तकों के ऊँचे दामों से खीझे हुए पाठक और वाम के हाथ बिके लेखक, दोनों की ही प्रतिक्रिया बड़ी जोरदार होती है। लेखक पाठक की नासमझी पर तरस खाता है कि वह इस संघर्ष में साझीदारी क्यों नहीं करता और पाठक, लेखक के प्रभामंडल को धुंधला करता हुआ कहता है – हैलो कामरेड! यह ट्रेजेडी आज हिन्दी साहित्य को खाए जा रही है।
‘दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ’, यह नारा दिया था एक आप्त पुरुष ने मजदूरों के लिए और काम आया हिन्दी के लेखकों के। और इस नारे की खूबी देखिए कि क्योंकि यह नारा मजदूरों के लिए था तो हिन्दी के लेखक इतिहास में शायद पहली बार मजदूर हुए। एक मेहनतकश इंसान। मेहनत ही जिसका धर्म है। मेहनत ही जिसकी पूँजी है। और साहित्यिक रचनाएं मेहनत बनाम पूँजी होकर रह गईं। अब ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि मेहनत से बनता है मेहनताना, सो मेहनत की तो मेहनताना भी चाहिए और दुर्भाग्य यह देश का कि मेहनताना अब भी पूँजीवाद के हाथ में है। परिणाम यह हुआ कि पूँजीवादी अपनी एक पत्रिका या प्रकाशन का परचम लहराता है और ये मेहनतकश वहाँ अपनी रचनाएं भेज कर मेहनताने के चेक की आस संजोते हैं और इस प्रकार पूँजीवाद का हित साधते-साधते ये स्वयम् उसी तंत्र का एक अंग बन जाते हैं। समझदार के लिए उनकी यह बेइमानी भी कम चटखारा लेने के लिए नहीं कि अपनी रचनाओं में जिस भूख-पसीने, जिस जर्जर जवानी का, सूनी आँखों से तकते हुए जिस भविष्य का ये जीभर जिक्र करते हैं, वह सब इन्हें छू तक नहीं जाता। परिसंख्या का प्रयोग करने की छूट यदि शीतल प्रसाद को दी जाए तो वह कहेगा – भूखे ये एकादशी जैसे व्रत में रहते हैं(दिन भर पारायण के प्रसाद की तैयारी की खुसबू में मस्त) घायल ये शेव के समय सिर्फ विदेशी ब्लेड की धार से होते हैं(चमचमाती टेबुल पर आफ्टर शेव लोशन या ‘फारमैन क्रीम’!) और अपने शरीर को नंगा ये धूप स्नान में या देश-काल विशेष में ही देख पाते हैं। गरीबी, इनके यहाँ एक हथियार है, नियति नहीं जिससे ये अपने आस-पास गरीबी को फटकने नहीं देते। गरीब इनके यहाँ इनकी दया का पात्र नहीं इनकी कहानी का पात्र है। भूख, पसीना, गरीबी जैसे शब्दों से खिलबाड़ करने वाले ये बुद्धिजीवी जिस तरह इस सबको कैश करते हुए बेसम्री से इसका विलोम जीते हैं वह वास्तव में तो लज्जास्पद कम और घ्रणास्पद अधिक है। वह बेचारा गरीब जो इनकी ‘कैशक्राप’ है तो इनको कभी देख ही नहीं पाता। अगर एक पुराने शेर में एक मज़ाकिया तरमीम कर दी जाए तो उस गरीब की आवाज कुछ ऐसी ही सुनाई पड़ेगी –
‘हम ही उनको वाम पै लाए
दीद से हम महरूम रहे।’
साहित्य की चर्चा हो और नारी अचर्चित रह जाए, ऐसा किसी युग में नहीं हुआ। समाज में नारी, पुरुष के साथ अनेक सम्बन्धसूत्रों से जुड़ी हुई है और साहित्य सम्पूर्ण समाज के दर्पण होने का दावा पहले ही पेश कर चुका है। नारी-पुरुष सम्बंधों में प्रेम(जिसे लाड़ में सूखे होठों पर जीभ फेर कर ‘पिरेम’ कहा जाता है) की भूमिका बड़ी मारक और महत्त्वपूर्ण है। भक्तिकाल में तो खैर नारी को माया के रूप में महाठगिनी देखते हुए सन्तकवि अपने एकतारे पर निर्गुण गाकर शून्य शिखर से झरते हुए अमृत रस को पीते रहे और रीतिकाल में कहते हैं कि नारी को सिर्फ भोग्या मान लिया गया। छायावाद बेचारा अपने ऊपर ‘स्त्रैणता’ का लेबिल लगवाकर गायब हुआ पर समाज के इस ‘शोषित वर्ग’ के सबसे बड़े हिमायती इन वाम साहित्यकारों की दैनन्दिनी भी इस प्रसंग में बड़ी रसभरी है। प्रेम चन्द हादसों का मुन्तजिर हमेशा रहा है और कोई पुरोधा अपनी कुरूप पत्नी को घास छीलकर मृत्यु-द्वार तक पहुँचने पर बाध्य कर अक्षता विधवा से विवाह कर क्रांतिकारी बना तो किसी लीला पुरुष ने अपनी ब्याहता को पत्थरों में फेंक दिलफेंक तरीके से किसी परी को रानी बनाया। ठेठ पूरब के गंवई गाँव से निकला भूस्पर्शी कुर्ता धारण करने वाला कोई वाम-चिन्तक जब किसी शक्ति-पुत्र का कृपा भाजन बन कर महानगरीय परिवेष में पहुंचा तो अपनी हीनग्रंथि से मुक्त होने के लिए उसने जहाँ भूस्पर्शी कुर्ते को काटते-छाँटते कटि-प्रदेश तक पहुंचाया वहाँ ‘यूडी कालॉन’ पर भी कब्जा किया। नारी-मुक्ति के जबर्दस्त हिमायती इन चिन्तकों की धर्मपत्नियाँ रेत की मछली बनकर रह गईं और ये सौन्दर्यशास्त्र की क्रियात्मक व्याख्याएं करने लगे।
पुरुष कोटि के साहित्यकार ने यह प्रगति-शीलता नारी के प्रति दिखाई तो भला इस कोटि की महिला साहित्यकार पीछे कैसे रहतीं। ऐसे-ऐसे चटखारे लेखिकाओं ने अपने लेखन में लिए कि अंग्रेजी का ‘बोल्डनैस’ शब्द अपना पूरा अर्थ खोलने लगा। सूरजमुखी अंधेरे में खिलने लगे और शब्दों की जादूगरी कि बलात्कार कविता में ढलने लगा। कहीं लेखिका एक नन्हें-मुन्ने उपन्यास में कई पृष्ठों में नायक के उद्दाम मनोरथ को खोलती चली गई कि काश! उसकी एक जीभ के स्थान पर असंख्य जीभें होती जिनसे न जाने वह कहाँ-कहाँ से नारी की देहयष्टि के रस को आत्मसात् कर लेता। सचमुच वहाँ वाम एक आन्दोलन जान पड़ता है, ऐसा आन्दोलन जो आन्दोलित करता चला जाए। वामा खुद वाम के लिए एक टॉनिक बनी।
प्रतिबद्धता स्वयम् में कोई बुरी चीज नहीं किंतु साहित्य के संदर्भ में इस शब्द का एक दार्शनिक पहलू भी है। यूं तो अगर इस शब्द का प्रयोग न भी किया जाए तो भी प्रत्येक लेखक प्रत्येक काल में एक प्रतिबद्ध लेखन ही करता है और वहाँ उसकी प्रतिबद्धता होती है कला सम्बंधी अपनी संवेदना के प्रति। अपने कला-संस्कारों अहसास के प्रति। अत: प्रतिबद्धता स्वत: सिद्ध कोई पदार्थ नहीं। वह परत: सिद्ध है। वाम लेखन में यह एक वस्तु-विशेष या भाव-विशेष के लिए जैसे मानों रूढ़ ही हो गया और लेखकों की एक जिद की तरह उभरा। ‘रस’ जैसे प्राचीन शब्द के प्रयोग से ये लेखक भले ही नाक-भौं सिकोड़ें किन्तु वह अब भी साहित्य का पर्याय ही है और उस दशा में भला आप किसी खास किस्म के रस को अपनी प्रतिबद्धता के तहत लाजिम करार कैसे दे सकते हैं। अब यह तो सनक ही कही जाएगी कि कोई वरिष्ट लेखक घोषणा कर दे कि अच्छा रस खट्टा होने के लिए बाध्य है। यहाँ ‘रस’ और ‘खट्टा’ के अन्वय-व्यतिरेकी सम्बंध के साथ उसका पूर्वग्रह स्वयं सिद्ध है। और तब उस दशा में प्रश्न यह भी उठेगा कि शेष रस क्या करेंगे। ‘भिन्नरुचिर्हिलोक:’ की कहावत अपना अर्थ कहाँ पाएगी।
तख्ती पर बालक को हाथ पकड़ कर लिखने का अभ्यास कराया जाता है। कुछ समय बाद तख्ती पर कोई बड़ा पेन्सिल से अक्षर बना देता है और बालक उन अक्षरों पर खड़िया से लिखता है। लेकिन ये अभ्यास की स्थितियां हैं। कालान्तर में सहायक का हाथ और पेन्सिल के अक्षर गायब हो जाते हैं और अब वह उन अक्षरों को किसी भी प्रकार लिख सकता है, बस अक्षरों का कैरेक्टर बना रहना चाहिए। अक्षर अर्थात् कैरेक्टर। लेकिन भाषा के कैरेक्टर और अपने कैरेक्टर में एक समान्तर दूरी रखने वाले लेखक का तो मामला ही और है। एक बूढ़े ऋषि ने पेन्सिल से एक अक्षर लिख दिया – वाम। और सरस्वती के वरदपुत्र ये उसी पर खड़िया से लिखते चले आ रहे हैं, सम्पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ। यह प्रतिबद्धता विश्व साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ ही है।
यह प्रतिबद्धता लेखन-प्रक्रिया में कुछ इस प्रकार उतरती है। एक सैट फारमूले पर ये वाम कहानी की बुनावट(रचना नहीं) होती है। प्रारम्भ : एक अभाव का अंकन, गरीबी और बेबसी। आरोह : यह गरीबी क्यों है? एक ऐतिहासिक चिंतन, चरमस्थिति : कारण की खोज। पड़ताल। खलनायक या एटी हीरो का उदय। यह कोई व्यक्ति हो सकता है और वर्तमान व्यवस्था भी। अवरोह : संघर्ष। इसमें अधिकार की व्याख्या की जाती है।(नागरिक शास्त्र के अध्येताओं को यहाँ बहुत कुछ मिल सकता है। यहाँ वे अपनी इन मान्यता को सुधार सकते हैं कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ का सिक्का एक पहलू का है। अधिकार का पहलू। वाम का सिद्धांत अधिकारों की लड़ाई के लिए है, कर्तव्य का दकियानूसी कीर्तन करने के लिए नहीं।) और अंतत: इसमे नायक शानदार कामयाबी हासिल करता है। उसका तो जन्म ही कामयाबी के लिए होता है अन्यथा उसे इस भवबाधा में फंसने की भला क्या आवश्यकता थी? नायक कोई भी हो सकता है, चिथड़े-चिथड़े समाज का टूटा-हारा कोई क्रांतिपुत्र – एक नया अभिमन्यु या प्रतीक की उंगली पकड़े चार दिन से भूखा-प्यासा एक कमरे में बंद बिल्ला। और वह बिल्ला कहानी के अंत में अपनी भूख-प्यास से उर्जा ग्रहण करके कमरे में उछलेगा, रोशनदान तोड़ेगा, बाहर आएगा और धूप सेकेगा। अब पाठक बेचारगी से अगर सोचे कि उस भूखे-प्यासे जर्जर बिल्ले की क्या बिसात कि रोशनदान तोड़ कर बाहर आ जाए तो लेखक की दृष्टि से पाठक में समझ का अभाव है। उसे नहीं भूलना चाहिए कि सम्भव-असम्भव की स्थितियां तो साधारण जन के चोंचले हैं। कहानी का बिल्ला एक प्रतीक है, सब कुछ करने में समर्थ और कहानी का लेखक एक प्रतिबद्ध लेखन से जुड़ा आप्त पुरुष है। कुछ सन्देह नहीं किया जाना चाहिए। वह दबे, थके अपने प्रतीक तक को हारा हुआ नहीं देख सकता। आप्त-प्रमाण की तरह उसका चिन्तन भी परम प्रामाणिक है।
आलोचना के सिद्धांतों की कसौटी पर किसी साहित्य की परख होती है। अपनी रचनाओं के मूल्यांकन के लिए भी इन्हें कहीं जाना नहीं। किसी सिरफिरे ने अगर साहित्य के मानकों पर इन्हें कस दिया तो उसे ‘प्राध्यापकीय आलोचना’ कह कर नकार दिया। जब नया लिख रहे हैं तो मानक भी नए चाहिए ना! तो हाजिर हैं – नए प्रतिमान। नया व्याकरण। आलोचकों का भी एक अपना परिवार है और आलोचक हैं कि कविता का व्याकरण लिख रहे हैं। भोलेपन का यह अंदाज कि कक्षा ६ के छात्र की समझ से भी नीचे जा कर व्याकरण का सम्बंध भाषा से हटाकर कविता से जोड़ रहे हैं। एक ऊँची बाट कह रहे हैं। बात कोई ऊँची या नीची थोड़े ही होती है, उस बात को कहने वाला ऊँचा या नीचा बनाता है। कभी किसी आलोचना पुस्तक का नाम आएगा कहानी/कविता पर एक बहस। पूरी किताब में एक लेखक के कुछ निबंध। एक पात्री बहस। है न चकराने वाली बात? लेकिन चकराने का जिम्मा तो पाठक का ही है न कि लेखक का। सो पाठक तो बेचारा जन्मा ही चकराने के लिए है। हर लेखक अपना एक आलोचक तलाशता है और वह आलोचक उसके लिए अपरिहार्य हो जाता है। टांग टूटे अपाहिज की बैसाखियों की तरह और उस सहारे से बेचारगी से भरा लेखक यश के सुमेर के शिखर चूमना चाहता है। अपने पारिश्रमिक पर दृष्टि जमाए हुए आलोचक की दशा भी कमोवेश ऐसी ही है। और हा, ये आलोचक और ये लेखक जब किसी रेस्तराँ या काफी हाउस में बैठ कर स्निग्ध वाणी से एक दूसरे के यश का वर्णन करते हैं, कलम की तारीफ करते हैं तो शीतल प्रसाद स्वयं को उसी भावलोक में पाता है जहाँ एक स्थिति-विशेष में एक संस्कृत कवि ने स्वयम् को पाया था – अहो रूपमहोध्वनि: ।
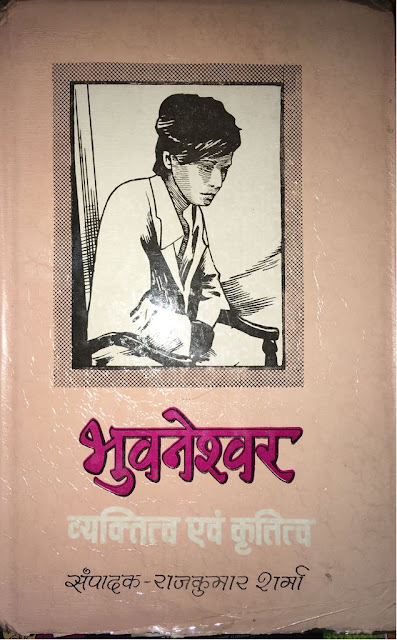
Comments
Post a Comment