पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य ‘त्रिपुरा’
पूर्वोत्तर
प्रदेश का जिक्र आते ही हमारे मनोमस्तिष्क में वहाँ की ऊँची-नीची पहाड़ी भूमि जो
सघन जंगलों से आक्षादित है तैरने लगती है। साथ ही मन में उठने लगती हैं ब्रह्मपुत्र
और उसकी सहायक नदियों की मन को मोह लेने वाली उत्ताल तरंगें। इस प्रदेश में जहाँ
एक ओर सिक्किम की बर्फ से ढकी और सैलानियों के साथ हँसती-खिलखिलाती सूर्य की
लालिमा से चमकती हुई पहाड़ियां हैं तो दूसरी ओर असम का कामाख्या मंदिर और रिमझिम
बारिश से मन को मोहने वाले प्रदेश। ऐसा ही मन को मोहने वाला एक छोटा राज्य है
त्रिपुरा, जहाँ का इतिहास और भौगोलिक वातावरण उसे कई मायनों में महत्त्वपूर्ण
बनाता है।
प्रथमत:
बात की जाए इस राज्य के नाम ‘त्रिपुरा’ की, जिसकी जड़े तलाशते हुए विद्वान तमाम
अटकलें लगाते रहे हैं। तमाम जनश्रुतियां प्रचलित हैं इस नाम को लेकर। कोई इस नाम
को बर्बर राजा ‘त्रिपुर’ से जोड़ता है तो कोई इसे ‘शिव/त्रिपुरारी’ से संबद्ध करके
देखता है। आगे तो विद्वानों ने शिव-पत्नी ‘त्रिपुर-सुंदरी’ अथवा ‘त्रिपुरेश्वरी’
से इस नाम का संबंध दिखाया। कुछ विद्वानों ने इसको तिब्बती-बर्मी और चीनी-तिब्बती
भाषा परिवार से जोड़ते हुए काकबरक भाषा के दो शब्दों ‘तुइ’ और ‘प्रा’ अथवा ‘तुइ’ और
‘बुप्रा’ उत्पन्न बताया। यहाँ पर ‘तुइ’ का अर्थ है ‘पानी’ और ‘प्रा’ का अर्थ है
‘निकट’। इस प्रकार तात्पर्य निकला ‘पानी के निकट’। महादेव बर्मन के अनुसार कहें तो
– “...पुराने समय में, शायद, त्रिपुरा की सीमाएं समुद्र तक या बंगाल की खाड़ी तक
जाती हों। त्रिपुरा के लोग मूलत: मंगोल नस्ल के हैं और आरंभिक संस्कृत पाठों में
मंगोल को सामान्यत: ‘किरात’ कहा गया है। पुराकथाओं के अनुसार, तिब्बत के कैलास
पर्वत पर रहने वाले भगवान शिव ने किरात रूप धारण किया था और हिमालय में अर्जुन से
लड़ाई की थी। सुनीति कुमार चटर्जी ने अपने महान ग्रंथ ‘किरात-जनाकृति’ में इस पूरी
कथा और उसके निहितार्थों का विश्लेषण किया है।”
वस्तुत:
हजारों वर्षों से पल्वित-पुष्पित हो रहे इस राज्य का शासन-प्रबंध बरोक/बरॉक अथवा
तिप्रा राजाओं के हाथों में रहा। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हुआ
त्विप्रा(त्रिपुरा) को 15 अक्टूबर 1949 को
भारतीय गणतंत्र में सम्मिलित किया गया था। महाभारत, योगिनी तथा कालिका आदि पुरातन
ग्रंथों में उल्लिखित इस नाम के बारे में अनेकानेक कहानियाँ यहाँ के जनसामान्य में
आज भी पाई जाती हैं। सितंबर 1956 को राज्यों के पुनर्गठन के
समय इस राज्य को केन्द्र शासित राज्य बनाया गया और 21 जनवरी 1972
को त्रिपुरा को विधिवत् एक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ।
त्रिपुरा
में मुख्य रूप से दो समुदायों का निवास स्थान है – बंगाली और जनजातीय। जनजातीय
समाज में यहाँ उन्नीस प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं – त्रिपुरी अथवा देवबर्मा,
रियांग, जमातिया, नोवातिया, चकमा, हालाम, मोग, लुशाई, उचई, कूकी, गारो, मुंडा,
भील, ओरांग, संथाल, खासी, चमैली, भूरिया एवं लेप्चा। इन दो समुदायों के आधार पर ही
यहाँ मुख्य रूप से दो भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं – बंगला एवं काकबरक। बंगला
यहाँ की प्रथम राजभाषा है जबकि काकबरक को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है।
स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा का माध्यम भी बंगला ही है। इन भाषाओं के
अतिरिक्त यहाँ अंग्रेजी और हिन्दी भी बोली-समझी जाती है। लेखन के लिए मुख्य रूप से
बंगला और रोमन लिपि अपनाई गई है। देवनागरी लिपि केवल केन्द्रीय विद्यालय,
महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के हिन्दी विभागों तक ही सीमित है लेकिन इधर अगरतला
में जब से ‘त्रिपुरा विश्वविद्यालय’ को ‘केन्दीय विश्वविद्यालय’ का दर्जा मिला है
तब से हिन्दी का प्रयोग अपनी उन्नति को सूचित करने लगा है।
त्रिपुरा
को जानने-समझने के क्रम में सबसे अहम है यहाँ के भौगोलिक वातावरण को समझना। वास्तव
में देखा जाए तो त्रिपुरा एक पर्वतीय राज्य है। पहाड़ियों-घाटियों से घिरे इस राज्य
में छ: प्रसिद्ध पहाड़ियों की चर्चा होती है – जम्पुई, शखांतलांग, लोंगतोराइ,
अथरमुरा, भाशमुरा और देवतामुरा। यह पहाड़ियां अधिकांशत: चिकनी मिट्टी और रेत की हैं
जिनमें तेल और गैस के भंडार हैं। गुवाहाटी से राजकीय राजमार्ग संख्या 44 से जुड़े त्रिपुरा राज्य की सीमा बंगलादेश के साथ 856 किमी. है जो कि कुल सीमा का 84% है और बंगलादेश की
राजधानी ढाका करीब-करीब यहाँ से 150 किमी. के दायरे में आते
हैं, जबकि प्रदेश की राजधानी अगरतला से कोलकाता की बंगलादेश से होते हुए दूरी 350
किमी. है। यहाँ पर यातायात के मुख्य रूप से दो प्रमुख साधन हैं – बस
और वायुयान, क्योंकि रेलों का विकास अभी उतना नहीं हो पाया है। रेल के नाम पर महज
एक ही छोटी रेलवे लाइन है जो लामडिंग(असम) से अगरतला को जोड़ती है। भूस्खलन आदि के
चलते या अन्य कारणों से यह लाइन अक्सर बाधित भी रहती है।
इस
राज्य का कुल क्षेत्रफल 10,492 वर्ग किमी. है(देश का तीन सौंवा
हिस्सा), जिसमें 60% जंगल और पहाड़ हैं जबकि खेती योग्य भूमि
महज 27% ही है। चूँकि यहाँ औसत से करीब 210 सेटीमीटर अधिक वर्षा होती है इसलिए मुख्य फसल ‘धान’ है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ की
जनसंख्या 32 लाख है जो पूर्वोत्तर भारत में असम के बाद दूसरे
स्थान पर है। नदियों का यहाँ विशेष स्थान है क्योंकि यहाँ का मुख्य आहार मछली है।
यहाँ की सबसे बड़ी नदी ‘मेघना’ है जबकि लोंगाइ, जूसी, मनु, देव, घलइ, खोवाइ, हावड़ा,
गोमती, मुहाटी तथा फेनी आदि अन्य प्रमुख नदियां हैं।
त्रिपुरा
का महत्त्व इसकी वनस्पतियों को लेकर भी है। कर्क रेखा पर स्थित इस राज्य में
वनस्पतिशास्त्रियों द्वारा पेड़-पौधों, झाड़ियों-लताओं आदि की तकरीबन तीन हजार
किस्में बताई गई हैं। इस दृष्टि से यह देश का आठवां हिस्सा नजर आता है।
वनस्पतिशास्त्रियों द्वारा किए गए तमाम अध्ययनों के आधार पर अब तक यहाँ करीब-करीब 266 प्रकार की वनस्पतियों की खोज की जा चुकी है, जिनमें अर्जुन, आंवला, नीम,
बहेड़ा, पलास, सर्पगंधा, बेल, हर्तकी, अश्पेक, वनतुलसी, ब्राह्मी, हरती, चित्ता,
नागेश्वर आदि। इस पर प्रकाश डालते हुए श्री एच. सी. गेना कहते हैं-“... राज्य में
केन्द्रीय सरकार की योजना ‘अकाष्ठ वनोपजमय औषधीय पौधे’ के अंतर्गत बंजर वनभूमि पर 505 हैक्टेयर औषधीय पौधे(अर्जुन, बहेड़ा, पलास, हर्तकी, आमला, नीम आदि) लगाए
गए। त्रिपुरा राज्य औषधीय एवं सुगंधित
पौधों के उत्पादन में अग्रणी है। इस राज्य में औषधीय एवं सुगंधित पौधे बहुतायत में
पाए जाते हैं, अत: यहाँ उनसे संबंधित उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लिए अनुकूल
वातावरण है। राज्य में औषधीय पौधों के उद्योगीकरण के क्षेत्र में संभावनाओं को
खोजने, संरक्षण व मूल्य वृद्धि के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यहाँ
पर इस क्षेत्र में निवेशकों के लिए व्यवसाय की बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि राज्य
में औषधीय पौधों का खजाना उपलब्ध है।
राज्य
में जैव विविधता का सूचकांक 5.23 है जो सामान्यत: 3-4 ही
होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि त्रिपुरा हमारे देश में जैव विविधता में धनी
राज्य है। राज्य में जैव-विविधता पत किए गए अध्ययन में कुल 379 वृक्ष प्रजातियां, 320 झाड़ी प्रजातियां, 581 जड़ी-बूटियां, 165 लता प्रजातियां, 16 लता-झाड़ी प्रजातियां, 35 फर्न प्रजातियां, 45
इपिफाईटस एवं 4 परजीवी प्रजातियां पायी गयीं। इनमें 50 पौधों की प्रजातियां ऐसी हैं जो केवल त्रिपुरा एवं उसके आस-पास के राज्यों
में पायी जाती हैं। इनमें से 7 प्रजातियां विलुप्त होने की
श्रेणी में हैं तथा 18 पौधे दुर्लभ पौधों की श्रेणी में आते हैं।
राज्य
के तृष्णा अभ्यारण्य में वनस्पतियों की दुर्लभ प्रजातियां जैसे फर्न की Angiopteris
evecta एवं लता की Gneteum montanum बहुतायत
से पायी जाती हैं। इसी प्रकार Cyathia spp. जो बहुत ही
दुर्लभ व लुप्त प्राय प्रजाति है, दक्षिण त्रिपुरा में पायी जाती है।
यहां
आर्किड की कुल 24 प्रजातियां हैं जिसमें से अकेले Dendrobium
की 14 प्रजातियां पायी जाती हैं। राज्य आर्किड
की लुप्तप्राय प्रजातियां जैसे Blue vanda तथा Red vanda भी पायी जाती हैं।”
उक्त
के अतिरिक्त यहाँ की कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जिन्हें यहाँ का जनमानस सामान्य रूप
से प्रयोग करता है। जैसे; बंदरताला(हृदयरोग के लिए उपयोगी), सीकी तांग पौधा(हड्डी
के दरकने पर प्रयोग में लाया जाता है), मुइका डोकला(गले के दर्द के लिए),
दूओरंग(सरदर्द के लिए उपयोगी), उआबामथू(पायरिया के लिए), जोबामफ़ाग(जोड़ों में सूजन
के लिए) आदि। कुल मिलाकर यहाँ की सामान्य चिकित्सा पद्धति वनस्पति पर ही आधारित
है।
औषधीय
रूप में प्रयुक्त किए जाने के अतिरिक्त यहाँ कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जिनसे यहाँ के
कुछ विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं; जैसे – ‘किचिरी’ नामक वनस्पति से एक विशेष प्रकार
का व्यंजन ‘गुडक’ बनता है तो ‘मुइखुम चाक’ से ‘लो इतका’ नाम का व्यंजन बनाया जाता
है। “गडरूई’ नामक वनस्पति से ‘बेरामा बटूई’ नामक व्यंजन बनाया जाता है तो
‘बाइकांग’, ‘खमका सीकुम’, ‘खमका’, ‘ थागंगा’, ‘कलमी हाक’, ‘चुपूई’, ‘पाचक’ आदि
तमाम वनस्पतियों से विशेष अवसरों पर तमाम प्रकार के विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं।
इन
वनस्पतियों पर प्रकाश डालते हुए श्री धीरंजन मालवे कहते हैं कि “इस दिशा में कुछ
कार्य हुए हैं। असम विश्वविद्यालय, सिलचर के जीन विज्ञान विभाग के दो वैज्ञानिकों,
एस. शील और एम.दत्त चौधरी ने त्रिपुरा की रियांग जनजाति के पास संचित औषधीय ज्ञान
पर एक शोधपत्र प्रकाशित किया है। रियांग त्रिपुरा की उन्नीस जनजातियों में एक है
और आबादी के हिसाब से दूसरे स्थान पर है। रियांग लोग त्रिपुरा के अत्यंत दुर्गम
घने जंगलों में रहते हैं और अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह इन्हीं जंगलों पर
निर्भर हैं। इनकी अपनी चिकित्सा पद्धति है जो जंगली वनस्पतियों पर ही आधारित है।”
त्रिपुरा
का इतिहास काफी पुराना है। यहाँ के इतिहास के मुख्यत: दो दौर रहे हैं – एक,
‘राजमाला में वर्णित पारंपरिक या पौराणिक काल’ और दूसरा, पन्द्रहवीं शताब्दी के
बाद का ऐतिहासिक काल।
राजमाला
एक ऐसी पुस्तक है जिसमें यहाँ के प्राचीन राजाओं के इतिहास को पन्द्रहवीं शताब्दी
के राजा धर्म माणिक्य के शासन काल के दौरान लिपिबद्ध किया गया था। जनश्रुति के
आधार पर इस पुस्तक को लिपिबद्ध किया था आदिवासी राजपुरोहित ‘दुर्लभेंद्र चंताई’ ने
और आगे चलकर राजदरबार के ही दो अन्य राजपुरोहितों –शुक्रेश्वर और बानेश्वर- ने
बंगला में अनुवाद किया था। इस पुस्तक की चर्चा बंगला भाषा और साहित्य की प्राचीनतम
किताबों में की जाती है। वस्तुत: यह काल और इसमें पाई जाने वाली पुस्तकें,
दंतकथाओं और पौराणिक कथाओं के आवरण में लिपटी हुई होने के बावजूद प्राचीन इतिहास
के महत्त्वपूर्ण स्रोत माने जा सकते हैं।
त्रिपुरा
के ऐतिहासिक काल का निर्धारण यहाँ पाए जाने वाले सिक्कों आदि पुरातात्विक नमूनों
के आधार पर किया जाता है। इन्हीं सिक्कों के आधार पर पता चलता है कि 15 अक्टूबर, 1949 को भारतीय
गणतंत्र में शामिल होने से पहले इस राज्य का शासक माणिक्य वंशीय राजा ही थे।
राजमाला
के आधार पर देखें तो त्रिपुरा के शुरुआती राजाओं का नाम वस्तुत: बोडो शब्द ‘फा’
अर्थात ‘पिता’ के साथ खत्म होता था लेकिन आगे चलकर ‘फा’ शब्द ‘माणिक्य’ में
परिवर्तित हो गया। महादेव बर्मन के अनुसार “राजमाला और दूसरे पुरातात्विक स्रोतों
से पता चलता है कि प्राक् औपनिवेशिक दौर में मिथिला और कान्यकुब्ज के ब्राह्मण
पुरोहितों को माणिक्य राजाओं ने अपने यहाँ आमंत्रित किया और त्रिपुरा के राजाओं ने
महाभारत के चंद्रवंशी ययाति के तीसरे पुत्र द्रुह्य से अपनी वंश-परंपरा की शुरुआत
का दावा किया। धार्मिक संस्थाओं के जरिये मध्यकालीन नरेशों द्वारा अपनी स्थिति की
वैधता सिद्ध करने का प्रयास विश्व के अनेक
हिस्सों में बहुत आम रहा है।” त्रिपुरा के राज दरबार की भाषा ‘संस्कृत’ थी जो
मध्यकाल में ‘पालि’ से होते हुए तुर्कों के आगमन के बाद अरबी-फ़ारसी और औपनिवेशिक
काल में अंग्रेजी हो गई। 1748 मे कृष्ण माणिक्य को हराकर शमशेर गाजी
त्रिपुरा का शासक हुआ लेकिन बंगाल के नबाब मीर कासिम के छलावे में आकर 1760
में मारा गया और एक बार फिर से त्रिपुरा का राजसिंहासन कृष्ण
माणिक्य के हाथ में आ गया।
अंग्रेजी
शासन के दौरान त्रिपुरा का विभाजन दो भागों में किया गया था – पहाड़ी(वर्तमान) और
जमीनी(वर्तमान बंग्लादेश का कोकिल्ला नामक स्थान)। इस समय इसका नाम ‘तिप्पराह’ था
जोकि 1920 में राजा बीरेंन्द्र किशोर माणिक्य के
शासन काल में अंग्रेज सरकार की रजामंदी से पहाड़ी तिप्पराह को त्रिपुरा नाम दिया
गया। 1965 में ईस्ट इण्डिया कंपनी को मिली बंगाल की दीवानी
के समय मुस्लिम-लगान-सूची वाला हिस्सा ब्रिटिश शासन के अधीन चला गया और ब्रिटिश
शासन के दौरान भी यह प्रदेश यहाँ के माणिक्य राजाओं के शासन में ही रहा। साथ ही एक
और स्थान ‘चकला रोशनाबाद’ के कुछ इलाकों की ज़मीदारी भी इन माणिक्य राजाओं को मिल
गई। इस दौरान इन शासकों ने गैरआदिवासी जातियों को अपने यहाँ स्थाई रूप से बसाया।
नतीजतन राजसी त्रिपुरा में गैर आदिवासियों के बसने की प्रक्रिया का आरंभ हो गया,
जो आगे तक बनी रही। धीरे-धीरे इस प्रक्रिया ने समस्या का रूप ले लिया और बीसवी सदी
में पूरा परिदृश्य बदल गया। समय के साथ यह समस्या और भी जटिल होती गई।
त्रिपुरा
का प्राचीन इतिहास आदिवासियों का इतिहास रहा है। आदिवासी ही तमाम श्रोतों के
अनुसार यहाँ के मूल निवासी माने गए, लेकिन प्रवासियों का आना जो एक बार आरंभ हुआ
था, बढ़ता ही गया और पूर्वोत्तर भारत में आज त्रिपुरा ही अकेला ऐसा राज्य है जो
अपने मूल आदिवासी रूप से बदलकर गैर आदिवासी रूप में अधिक पहचाना जाने लगा। इसका एक
कारण 1947 में देश के बटवारे के समय पूर्वी
पाकिस्तान(अब बंग्लादेश) से आए बंगाली शरणार्थी भी थे। महादेव बर्मन के शब्दों में
“1947 में बंगाल का अंतिम रूप से विभाजन त्रिपुरा के लिए एक
आपदा के समान था। इसने पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों के आगमन के लिए दरवाजे खोल
दिए जिसने अब तक की संरचना को हमेशा के लिए बदल दिया। जनसांख्यकीय परिवर्तन ने
यहाँ जातीय टकराव का मार्ग प्रशस्त किया जिसने पिछले तीन दशकों से इस छोटे से
राज्य को तबाह किया है। त्रिपुरा की आबादी 1921 में तीन लाख
थी। वह 2001 में बढ़कर बत्तीस लाख हो गई। 1949 में भारतीय संघ के अंतर्गत त्रिपुरा के विलय के बाद से बड़े पैमाने पर होते
हुए अप्रवासन के साथ कांग्रेसी सरकारों द्वारा सख्ती नहीं बरती गई तो उसका कारण था
वोट-बैंक की राजनीति। इस सिलसिले में आदिवासियों के हितों की लगातार अनदेखी हुई।”
अत: त्रिपुरा के आदिवासी जो कभी बहुसंख्यक थे, अल्पसंख्यक बनते गए। इसके कारण
आदिवासी और गैरआदिवासी जनसमुदायों के मध्य एक प्रकार की टकराव की स्थिति उत्पन्न
हो गई और इसी के साथ इस क्षेत्र में हथियारबंद विद्रोह आरंभ हो गया। देश की आजादी
के बाद भी त्रिपुरा तमाम सामाजिक, आर्थिक आदि स्तरों पर कठिनाइयों से लगातार जूझता
रहा।
वास्तव
में देखा जाए तो आज त्रिपुरा जिस रूप में है वहाँ तक पहुँचने के बीच कई संघर्ष
उसके इतिहास से जुड़े हैं। प्राचीन
विद्रोहों में 1850 का तिप्परा विद्रोह, 1860-61 का कुकी विद्रोह, 1863 का जमातिया विद्रोह और 1942-43
का रियांग विद्रोह आदि हलचल मचाते रहे तो राज्य को लोकतंत्र का
स्थान दिलाने के लिए भी कई विद्रोह हुए। 1938 में बारेन
दत्ता, प्रभात राय(देबबर्मा), बांगशी ठाकुर(अमरेंद्र देबबर्मा) आदि ने ‘जनमंगल समिति’
बनाकर वर्तमान राजा के सम्मुख एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए मांग रखी।
फलश्वरूप राजा द्वारा इस समिति को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बाद भी जब तक
त्रिपुरा को 1972 में स्वतंत्र राज्य का दर्जा नहीं मिल गया,
तमाम प्रकार के विद्रोह होते रहे। अंतत: ‘विभिन्न ऐतिहासिक आदिवासी विद्रोहों और
आदिवासी तथा गैरआदिवासी आम जनता के संयुक्त आंदोलनों के जरिए 1978 में पहली वाम मोर्चा सरकार का गठन हुआ और शाही रियासत रह चुके इस राज्य को
अंतत: आगे की पहलकदमियों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों का ईंधन हासिल हुआ।’
त्रिपुरा
का सामाजिक जीवन दो समुदायों का सामाजिक जीवन है। एक, बंगाली समुदाय और दूसरा,
जनजातीय समुदाय। इन दोनों समुदायों के अपने-अपने लोक-विश्वास और मान्यताएं हैं। इस
संबंध में यहाँ एक बात पर विशेष रूप से गौर किया जा सकता है। त्रिपुरा राज्य बंगाल
की सीमा में आता है और अपने इतिहास में, अंग्रेजों के आने से पूर्व, यह प्रदेश
अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता रहा है। कंपनी शासन के दौरान इस क्षेत्र को अनगिनत
बार लूटा गया और कई-कई बार पड़ने वाले अकालों ने इस क्षेत्र की कमर तोड़ दी। वसुत:
देखा जाए तो बंगाल प्रदेश यूरोप से सीधे जुड़ा रहा था। कहना न होगा कि नवजागरण काल
के दौरान यूरोप का काफी कुछ प्रभाव इस प्रदेश ने ग्रहण किया, लेकिन यहाँ पर एक बात
आश्चर्यचकित करने वाली यह है कि आज भी शेष भारत की तुलना में यहाँ पर यूरोपीय
संस्कृति का उतना प्रभाव नहीं दिखता है। यह प्रदेश अपनी लोक संस्कृति को आज भी सहेजे
हुए है।
पूर्वोत्तर
के मणिपुर, अरूणाचल, नागालैण्ड, मेघालय आदि करीब-करीब समस्त प्रदेश पश्चिम की छद्म
आधुनिकता के बड़े ही तेजी के साथ शिकार होते जा रहे हैं वहीं पहाड़ो-घाटियों,
नदी-नालों, झील-तालाबों आदि प्राकृतिक सुंदरता से घिरे इस प्रदेश के निवासियों ने
अपनी लोक संस्कृति को इस औपनिवेशिक वातावरण में सहेजा हुआ है। विभिन्न अवसरों पर
यहाँ पारंपरिक नाच-गानों की धूम हर समय सुनाई देती रहती है। यहाँ पर होने वाले
धार्मिक-सांस्कृतिक उत्सव भारतीय संस्कृति और लोक विश्वासों को बड़ी ही सहजता से आपके
सम्मुख प्रस्तुत कर जाते हैं।
यहाँ
के आदिवासी समाज में ‘गड़ियापूजा’ का विशेष प्रचलन है। सात दिनों तक चलने वाली इस
पूजा के समय किसी और देवी-देवता की पूजा नहीं की जाती है। डॉ. मिलनरानी जमातिया के
अनुसार इस पूजा के लिए “... पवित्र हरे बांस में पवित्र वस्त्र बांधकर सोने का
मुखौटा पहनाकर गाड़िया देवता का प्रतीक बनाते हैं।” यहाँ पर एक बात बताता चलूं कि
बांस का यहाँ विशेष महत्त्व है। इसका प्रयोग यहाँ जीवन की हर आवश्यकता के लिए किया
जाता है। जैसे; घर बनाने के लिए, बिछावन बनाने लिए, कुर्सी-मेल-बेड आदि बनाने के
लिए, खाने के लिए आदि। संभावत: जीवनदायक रूप में मानकर इसको देवता का प्रतीक बनाया
गया होगा। गारियापूजा के अतिरिक्त यहाँ के आदिवासियों में पर्वार की कुशलता के लिए
‘लाम्प्रा’, गांव और परिवार की सुरक्षा के लिए ‘केर नाकिरि’, व्यक्तिगत सुरक्षा के
लिए ‘नाक्सू’, धन-धान्य के लिए ‘माईलूमा-खुलूमा’, तांत्रिक कार्यों के लिए ‘बुरासा’,
वन के देवी-देवताओं की प्रसन्नता के लिए ‘थुनाईराग-बानेराग एवं हाईचुकमा’, राक्षसी
प्रजातियों से सुरक्षा के लिए ‘बोरोईराग’ आदि देवी-देवताओं की पूजा की जाती है और
साथ ही आदिवासी समाज में करीब-करीब समस्त हिन्दू देवी-देवताओं को भी पूजा जाता है,
लेकिन ये गौड़ रूप में आते हैं।
‘होजा
गिरि’ यहाँ का एक ऐसा नृत्य है जिसमें बंगाली और आदिवासी एक साथ दिखते हैं। यह एक
प्रकार की जनजातीय धुन है। इसके साथ ही ‘मानस-मंगल’ और ‘कीर्तन’ को बंगाली समाज
में प्रमुखता से अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त कबीलों में होने वाला ‘गाड़िया
नृत्य’ और बंगाली समाज में विशेषकर शादी-ब्याह के समय गाया जाने वाला एक विशेष गान
‘धमैल’ है। ‘धमैल’ एक प्रकार से कव्बाली की तर्ज का गान है जो दो दलों के बीच
प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाता है। यह आशु गायन है, क्योंकि इसकी रचना तत्काल
परिस्थिति के अनुसार की जाती है। ‘रवीन्द्र संगीत’ और ‘नज़रुल गीति’ भी यहाँ के
प्रमुख संगीत हैं। यहाँ पर ‘बुद्ध पूर्णिमा’ और ‘क्रिसमस’ जिस जोश और उत्साह के
शाथ मनाया जाता है उसी जोश और उत्साह के साथ मुस्लिम समुदाय के ‘जरी’ और ‘सारी’
नृत्य भी किए जाते हैं। जुलाई के महीने में जहाँ ‘चतुर्दश देवता’ का उत्सव सब
मिलकर मनाते हैं तो पांच दिनों तक चलने वाले दुर्गा पूजा की धूमधाम की जितनी
प्रशंसा की जाए कम है।
वास्तव
में त्रिपुरा के यह तीज-त्योहार और लोक संगीत इसकी उत्सवधर्मिता के द्योतक तो हैं
ही साथ ही यहाँ के समाज को जोड़ने वाली धुरी का काम भी करते हैं। विजय मोहन शर्मा
कहते हैं कि “इन त्योहारों को यहाँ के राजाओं का संरक्षण प्राप्त था और ये यहाँ के
भिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों को जोड़ कर रखने में इनकी भूमिका को समझते थे,
खासतौर से माणिक्य वंश के राजा जिन्होंने लगभग पांच सौ वर्ष तक राज किया। सचिन देब
बर्मन भी त्रिपुरा के राजघराने से थे, जो अपने बेटे राहुल देब बर्मन के साथ लगभग
पचास वर्षों तक फ़िल्मी दुनिया पर छाये रहे।” इतना ही नहीं अभी कुछ वर्षों पहले
आदिवासी लड़कियों का एक समूह ‘रंग’ के नाम से होली के समय अपने पारंपरिक नृत्य
‘होजागिरि’ की प्रस्तुति के लिए जापान भी गया था, जिसको जापान में बहुत पसंद किया गया।
बात जब
त्रिपुरा पर हो रही हो तब यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर ‘माताबारी’ और उन्नकोटि की बात न
करना बेईमानी होगा।
उदयपुर
जिले से चार-पांच किमी. दक्षिण में स्थित यह मंदिर त्रिपुरा की आस्था का सबसे बड़ा
प्रतीक है। पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र आता है। कहा जाता है कि मृत सती का एक
अंग यहाँ पर गिरा था, इस अर्थ में यह एक प्रकार का शक्तिपीठ है। वैसे यह स्थान एक
प्रकार की तांत्रिक आराधना का भी प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पर बकरे तथा भैंसे की
बलि का आज भी बहुतायत से प्रचलन है। इस मंदिर में जो मूर्ति है वह यहाँ की
स्त्रियों के नैन-नक्स पर आधारित है।
उन्नकोटि
में कहा जाता है कि एक कम एक करोड़ शिव की मूर्तियां हैं। यहाँ प्रचलित कथा के
अनुसार शिल्पकार द्वारा यह समस्त मूर्तियां एक ही रात में बनाई गई थीं। यह
मूर्तियां वस्तुत: वहाँ की पहाड़ियों पर उकेरी गई हैं। हर पहाड़ी, पत्त्थर एक मूर्ति
के आकार में है। इन मूर्तियों का चेहरा यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों के चेहरे से
मिलता है। कहना न होगा कि इन पहाड़ियों पर स्थित शिव आदिवासी समुदाय की अपनी मौलिक
कल्पना के प्रतीक हैं।
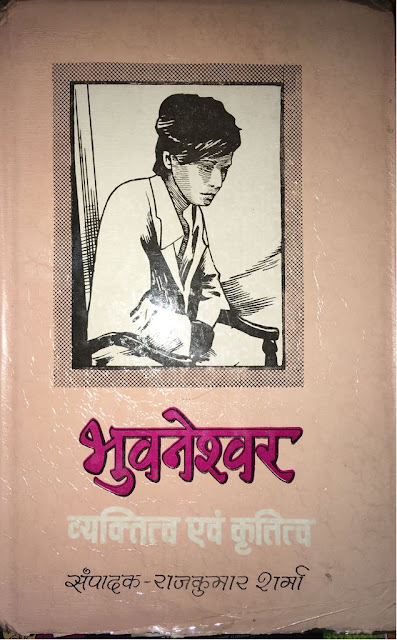
Comments
Post a Comment